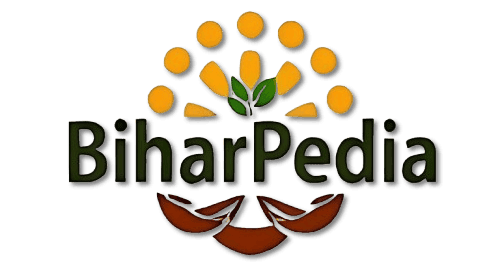धान की वैज्ञानिक खेती
धान भारत की एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है, जिसके सफल उत्पादन के लिए विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियाँ और कृषि पद्धतियाँ आवश्यक हैं। इस लेख मे विस्तृत जानकारी धान की वैज्ञानिक खेती के लिए एक मार्गदर्शिका प्रदान करती है, जिससे किसान अच्छी उपज और गुणवत्ता प्राप्त कर सकें।

जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी और रोपाई
जलवायु:
धान की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके पौधों के जीवनकाल में औसत तापमान 20-35 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए अच्छी वर्षा (या पर्याप्त सिंचाई) की आवश्यकता होती है।
मृदा:
धान की खेती के लिए मृदा का pH मान प्रायः 6.5-8.5 सर्वोत्तम होता है। इसके लिए अच्छी जलधारण क्षमता वाली मटियार या मटियार दोमट एवं चिकनी मृदा अच्छी मानी जाती हैं। हालांकि, सिंचाई की समुचित व्यवस्था तथा सही प्रबंधन से अधिकतर मृदा में धान की अच्छी पैदावार ली जा सकती है।
खेत की तैयारी:
- प्रारंभिक जुताई: गर्मी की जुताई के बाद 2-3 जुताइयां करके खेत की तैयारी करनी चाहिए।
- समतलीकरण और मेड़बंदी: खेत को समतल करने के साथ मजबूत मेड़बंदी भी कर देनी चाहिए, ताकि वर्षा का पानी अधिक मात्रा में संचित किया जा सके।
- रोपाई पूर्व तैयारी: धान की रोपाई के लिए एक सप्ताह पूर्व खेत की सिंचाई कर दें एवं रोपाई से पहले 2-3 जुताइयां हैरो से करें।
- पडलिंग: इसके बाद, पानी भरकर खेत में पडलर से जुताई करके एवं पाटा लगाकर मिट्टी को लेहयुक्त (puddled) एवं समतल बना दें। यह खरपतवारों को नियंत्रित करने और पानी के रिसाव को कम करने में सहायक होता है।
- मृदाजनित रोगों का प्रबंधन: इसमें 20-25 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा को 60 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद या वर्मीकम्पोस्ट में मिलाकर हल्के पानी का छींटा देकर एक सप्ताह तक छाया में सुखाने के बाद खेत में एक समान छिड़काव कर दें, जिससे मृदाजनित रोगों में कमी आएगी।
रोपाई:
- पौध की उपयुक्त आयु: इसके लिए 20-25 दिनों पुरानी पौध, जिसमें 4-5 पत्तियां हों, उपयुक्त होती है।
- रोपाई का समय:
- मध्यम एवं देर से पकने वाली प्रजातियों की रोपाई माह (जुलाई) के प्रथम पखवाड़े तक पूरी कर लेनी चाहिए।
- शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक पूरी कर लेनी चाहिए।
- धान की सुगंधित प्रजातियों की रोपाई माह के अंत में प्रारंभ करें।
- फसल चक्र और खाद: प्रत्येक वर्ष धान-गेहूं फसलचक्र अपनाने वाले क्षेत्रों में हरी खाद या 10-12 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें।
- पौध उखाड़ने से पहले: पौध उखाड़ने से एक दिन पहले क्यारी में अच्छी सिंचाई करें।
- रोपाई वाले दिन: रोपाई वाले दिन सुबह स्वस्थ, रोगमुक्त और शुद्ध किस्म की पौध को अलग करके 5-8 सें.मी. व्यास के नरम बंडलों में बांध लेना चाहिए।
- रोपाई की दूरी और गहराई: रोपाई 20-30 सें.मी. (कतार से कतार) x 15 सें.मी. (पौध से पौध) की दूरी पर करें। 3 सें.मी. की गहराई पर एक जगह पर 2-3 पौधे ही लगाएं।
- देर से या ऊसर मृदा में रोपाई: देर से अथवा ऊसर मृदा में रोपाई करने की अवस्था में, रोपाई के लिए लगभग 35-40 दिन पुरानी पौध को 15 सें.मी. x 10 सें.मी. की दूरी पर 3-4 पौधों के समूह में प्रत्येक स्थान पर लगाएं।
पोषक तत्व प्रबंधन और खरपतवार नियंत्रण
धान की खेती में अधिकतम उपज और स्वस्थ पौधों के लिए संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और प्रभावी खरपतवार नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी का प्रयोग :
| खरपतवारनाशी | सक्रिय तत्व | मात्रा/हैक्टर | प्रयोग का समय | खरपतवारों पर नियंत्रण |
|---|---|---|---|---|
| पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल (10 प्रतिशत) | 20 ग्राम | 200 ग्राम | रोपाई/बुआई के 3 दिनों के अन्दर | मोथाकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| बिस्पायरीबैक सोडियम (10 प्रतिशत) (नोमिनी गोल्ड) | 25 ग्राम | 250 मि.ली. | रोपाई/बुआई के 17-20 दिनों बाद | घासकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| एनीलोफोस (एनीलोगार्ड) | 400-500 ग्राम | – | बुआई/रोपाई के 3-4 दिनों बाद | घास एवं मोथाकुल के खरपतवार |
| प्रेटिलाक्लोर (37 प्रतिशत) | 555 ग्राम | 1500 मि.ली. | बुआई के 3 दिनों के अन्दर | घासकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| बेन्सल्फ्यूरॉन मिथाइल (0.6 प्रतिशत)+ प्रेटिलाक्लोर (6 प्रतिशत) | 6+600 ग्राम | 10 किग्रा. | रोपाई के 8 दिनों के अन्दर | घासकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| पेण्डीमेथिलीन (30 प्रतिशत) | 750-1000 ग्राम | 2.5-3.3 ली. | बुआई के 3 दिनों के अन्दर | घासकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| पिनाकुलसुम (1.02 प्रतिशत)+ साइहैलोफोप ब्यूटाइल (5.1 प्रतिशत) | 135 ग्राम | 2250 मि.ली. | बुआई के 20 दिनों बाद | घासकुल, मोथाकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| फेनाक्जाप्राप (5 प्रतिशत)+ इथाक्सी सल्फ्यूरॉन (15 प्रतिशत) | 60+20 ग्राम | 667 मि.ली.+ 135 ग्राम | बुआई के 20 दिनों बाद | घासकुल, चौड़ी पत्ती एवं मोथाकुल |
| फेनाक्जाप्राप पी-इथाइल (9 प्रतिशत) | 60 ग्राम | 667 मि.ली. | बुआई के 25 दिनों बाद | घासकुल |
| मेट्सल्फ्यूरॉन मिथाइल (10 प्रतिशत)+ क्लोरीम्यूरॉन इथाइल (10 प्रतिशत) | 4 ग्राम | 20 ग्राम | बुआई के 25 दिनों बाद | घासकुल एवं चौड़ी पत्ती |
| इथाक्सी सल्फ्यूरॉन (15 प्रतिशत) | 20 ग्राम | 135 ग्राम | बुआई के 20 दिनों बाद | घासकुल |
पोषक तत्व प्रबंधन:
- मृदा परीक्षण के आधार पर: उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के अनुसार ही करना चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी में पोषक तत्वों की वास्तविक स्थिति बताता है।
- बौनी प्रजातियों के लिए: सामान्यतः धान की बौनी प्रजातियों के लिये प्रति हेक्टेयर 100-120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 60 कि.ग्रा. पोटाश एवं 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट का प्रयोग कर सकते हैं।
- बासमती प्रजातियों के लिए: बासमती प्रजातियों के लिए प्रति हेक्टेयर 80-100 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50-60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 40-50 कि.ग्रा. पोटाश एवं 20-25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट देना चाहिए।
- उर्वरक प्रयोग का समय:
- सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश एवं जिंक की पूरी मात्रा आखिरी जुताई के समय देनी चाहिए।
- यूरिया की मात्रा को तीन भागों में बांटकर प्रयोग करें:
- एक तिहाई मात्रा: रोपाई के 5-8 दिनों बाद (जब पौध अच्छी तरह से जड़ पकड़ ले)।
- दूसरी मात्रा: 25-30 दिनों बाद (कल्ले फूटते समय)।
- तीसरी मात्रा: 50-60 दिनों बाद (फूल आने से पहले) खड़ी फसल में छिड़काव करें।
- जैविक खाद का प्रभाव: यदि हरी खाद या गोबर की खाद का प्रयोग किया गया हो, तो नाइट्रोजन की मात्रा 20-25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर तक कम कर सकते हैं।
जैव उर्वरक का प्रयोग:
- नील हरित शैवाल: नील हरित शैवाल की अधिकतर प्रजातियां प्रतिवर्ष लगभग 20-30 कि.ग्रा. नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मृदा में स्थापित करती हैं, जिसका प्रयोग धान की फसल द्वारा होता है।
- प्रयोग विधि: रोपाई के एक सप्ताह बाद, खड़े पानी में 10-15 कि.ग्रा. जैव उर्वरक प्रति हेक्टेयर की दर से बिखेर दें।
- नियमितता: शैवाल का प्रयोग कम से कम तीन वर्ष तक नियमित करें और ध्यान रखें कि खेत में पानी सूखने न पाए।
खरपतवार नियंत्रण:
- हानि: खरपतवार प्रायः फसल से नमी, पोषक तत्व, सूर्य का प्रकाश तथा स्थान के लिये प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे मुख्य फसल के उत्पादन में कमी आ जाती है। धान की फसल में खरपतवारों द्वारा 15-85 प्रतिशत की हानि आंकी गई है।
- प्रभाव: सीधे बोए गए धान की तुलना में रोपाई वाले धान में खरपतवार का प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है।
- पोषक तत्वों का शोषण: खरपतवार रोपाई वाले धान में 4-12 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 1-13 कि.ग्रा. फॉस्फोरस एवं 7-14 कि.ग्रा. पोटाश तथा सीधे बोये गये धान में 20-40 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 5-15 कि.ग्रा. फॉस्फोरस एवं 15-50 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से शोषित कर लेते हैं तथा धान की फसल को पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं।
इन वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर किसान धान की फसल में पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं और खरपतवारों से होने वाले नुकसान को कम करके अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं।
धान की फसल में रोग प्रबंधन
धान की फसल में विभिन्न प्रकार के रोग लग सकते हैं, जिनमें से लगभग 30 तरह के रोग केवल कवकजनित (fungal) हैं। फसलों की पैदावार और आर्थिक क्षति के दृष्टिकोण से, वर्तमान में देश में कुछ रोग विशेष रूप से गंभीर हैं।
धान के प्रमुख रोग:
1. बकानी रोग (Bakanae Disease)
- बकानी रोग, जिसे फुट रॉट भी कहा जाता है, धान की फसल का एक कवकजनित रोग है।
- रोग के लक्षण:
- प्राथमिक पत्तियाँ: रोग के प्रारंभिक लक्षणों में प्राथमिक पत्तियों का दुर्बल (कमजोर) तथा असामान्य रूप से लम्बा होना शामिल है।
- परिपक्व फसल में: फसल की परिपक्वता के समय, संक्रमित पौधे सामान्य से काफी ऊँचे, हल्के हरे रंग के और लम्बे टिलर्स (कल्ले) दर्शाते हैं।
- टिलर्स की संख्या: संक्रमित पौधों में टिलर्स की संख्या प्रायः कम होती है।
- पत्तियों का सूखना: रोग के बढ़ने पर, कुछ हफ्तों में ही नीचे से ऊपर की ओर एक के बाद दूसरी सभी पत्तियाँ सूख जाती हैं।
- जड़ों की स्थिति: संक्रमित पौधे की जड़ें सड़कर काली हो जाती हैं और उनमें दुर्गंध आने लगती है।
- रोग का नियंत्रण:
- इस रोग की रोकथाम के लिए कवकनाशियों (fungicides) के साथ बीजोपचार की संस्तुति की जाती है।
- बीजोपचार:
- कार्बण्डाजिम के 0.1 प्रतिशत (1 ग्राम प्रति लीटर पानी) घोल में बीजों को 24 घंटे तक भिगोएँ।
- इसके बाद बीजों को अंकुरित करके नर्सरी में बिजाई करें।
- पौध उपचार:
- रोपाई से पहले, पौध का 0.1 प्रतिशत कार्बण्डाजिम के घोल में 12 घंटे तक उपचार भी प्रभावी पाया गया है।
- ये उपाय बकानी रोग के संक्रमण को कम करने और स्वस्थ फसल सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
2. खैरा रोग (Khaira Disease):
- लक्षण: यह रोग जस्ते (जिंक) की कमी से होता है। निचली पत्तियाँ पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं और बाद में पत्तियों पर कत्थई रंग के छिटकवां धब्बे उभरने लगते हैं। इससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है।
- नियंत्रण:
- रोकथाम के लिए, रोपाई से पहले खेत की तैयारी के समय 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हैक्टर की दर से डालें।
- 5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट तथा 2.5 कि.ग्रा. चूना को 600-700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर छिड़काव करें।
3. पत्ती झुलसा रोग (Leaf Blight):
- लक्षण: यह रोग पौधे की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व होने तक कभी भी हो सकता है। इसके प्रकोप से पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्तों के साथ-साथ राख के रंग के चकत्ते भी दिखाई देते हैं, और बालियाँ दानारहित रह जाती हैं।
- नियंत्रण:
- रोकथाम के लिए, 74 ग्राम एग्रीमाइसीन-100 और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (फाइटोलॉन/ब्लाइटॉक्स-50/क्यूप्राविट) को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर की दर से 3-4 बार 10 दिनों के अन्तराल पर छिड़काव करें।
- बुआई से पहले बीज को स्ट्रेप्टोमाइसीन/एग्रामाइसीन से उपचारित करें।
- इस रोग के लगने पर नाइट्रोजन की मात्रा कम कर देनी चाहिए।
4. ब्लास्ट या झोंका रोग (Blast Disease):
- लक्षण: यह रोग फफूंद से फैलता है और पौधे के सभी भागों को प्रभावित करता है। प्रभावित पत्तियों पर भूरे धब्बे दिखाई देते हैं, जिनका बाहरी भाग कत्थई रंग का और बीच वाला भाग राख के रंग का हो जाता है। फलस्वरूप बाली आधार से मुड़कर लटक जाती है और दाने का भराव पूरा नहीं हो पाता। देर से रोपाई करने पर इस रोग का खतरा बढ़ जाता है।
- नियंत्रण:
- बीज को कार्बण्डाजिम एवं थीरम (1:1) की 3 ग्राम प्रति कि.ग्रा. की दर से उपचारित करना चाहिए।
- निम्नलिखित में से किसी एक दवा को 500-750 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर छिड़काव करें:
- कार्बण्डाजिम (50% डब्ल्यू.पी.) 500 ग्राम
- ट्राइसायक्लेजोल 500 ग्राम
- एडीफेनफॉस (50% ई.सी.) 500 मि.ली.
- हेक्साकोनाजोल (5.0% ई.सी.) 1.0 लीटर
- मैकोजेब (75% डब्ल्यू.पी.) 2.0 कि.ग्रा.
- जिनेब (75% डब्ल्यू.पी.) 2.0 कि.ग्रा.
- मैकोजेब (63% डब्ल्यू.पी.) 750 ग्राम
- आइसोप्रोथपलीन (40% ई.सी.) 750 मि.ली.
- कार्बण्डाजिम का 0.1 प्रतिशत की दर से दूसरा छिड़काव कल्ले फूटते समय और तीसरा छिड़काव बालियाँ निकलते समय ग्रीवा संक्रमण रोकने के लिए करना चाहिए।
5. झुलसा या पर्ण अंगमारी (Bacterial Leaf Blight):
- लक्षण: यह रोग जीवाणु द्वारा होता है और पौधे की छोटी अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक कभी भी हो सकता है। पत्तियों के किनारे ऊपरी भाग से शुरू होकर मध्य भाग तक सूखने लगते हैं। सूखे पीले पत्तों के साथ-साथ राख के रंग के चकत्ते भी दिखाई देते हैं। पत्तों पर जीवाणु के रिसाव से छोटी-छोटी बूंदें नजर आती हैं, पौधे में शिथिलता आ जाती है, और अंततः बालियाँ दानों से रहित रह जाती हैं।
- नियंत्रण:
- इस रोग के लगने पर नाइट्रोजन का प्रयोग कम कर दें।
- जिस खेत में रोग लगा हो, उसका पानी दूसरे खेत में न जाने दें।
- 74 ग्राम एग्रीमाइसीन-100 और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 500 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हैक्टर की दर से तीन-चार बार 10 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें।
- इसके अतिरिक्त, 15 ग्राम स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन (90%) या 15 ग्राम टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड (10%) को 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (50% डब्ल्यू.पी.) के साथ मिलाकर प्रति हैक्टर 500-750 लीटर पानी में घोल बनाकर 10-12 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करना चाहिए।
- रोग प्रतिरोधी प्रजातियों जैसे अजय, आईआर-42, आईआर-64 तथा स्वर्णा की खेती सर्वोत्तम तरीका है।
6. आवरण झुलसा (Sheath Blight):
- लक्षण: यह रोग फफूंद द्वारा होता है। पत्ती के शीथ पर 2-3 सें.मी. लम्बे हरे से भूरे रंग के धब्बे पड़ते हैं, जो बाद में भूसे के रंग के हो जाते हैं। इन धब्बों के चारों तरफ बैंगनी रंग की पतली धारी बन जाती है।
- नियंत्रण:
- निम्नलिखित में से किसी एक दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें:
- कार्बण्डाजिम (50% डब्ल्यू.पी.) 500 ग्राम
- थायोफिनेट मिथाइल (70% डब्ल्यू.पी.) 1.0 कि.ग्रा.
- कार्बण्डाजिम (12%) + मैंकोजेब (63% डब्ल्यू.पी.) 750 ग्राम
- प्रोपिकोनाजोल (25% ई.सी.) 500 मि.ली.
- हैक्साकोनाजोल (5.0% ई.सी.) 1.0 लीटर
- ट्राइकोडर्मा विरिडी 1% डब्ल्यू.पी. 5-10 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर पर्णीय छिड़काव करें।
- रोगरोधी किस्में जैसे कृष्णा सी. आर. 44-11, साकेत 1, पंकज, मानसरोवर आदि का चयन करें।
- निम्नलिखित में से किसी एक दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हैक्टर की दर से छिड़काव करें:
धान की फसल में कीट प्रबंधन
धान की फसल में कीटों के प्रकोप से न केवल उपज में कमी आती है, बल्कि गुणवत्ता भी प्रभावित होती है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है।
धान की फसल में वाले प्रमुख कीट:
1. पत्ती लपेटक (लीफ फोल्डर) कीट:
- क्षति: इस कीट की सुंडी पौधों की कोमल पत्तियों को किनारों से लपेटकर एक सुरंग बना लेती है और उसके अंदर पत्तियों को खाती रहती है। इससे पत्तियों का रंग उड़ जाता है और वे सूख जाती हैं।
- नियंत्रण:
- लाइट ट्रैप का प्रयोग करें।
- ट्राइकोग्रामा काइलोनिस (ट्राइकोकार्ड) 1-1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 30 दिनों बाद 3-4 सप्ताह तक छोड़ें।
- मोनोक्रोटोफॉस (36 डब्ल्यूएससी) 1.4 लीटर को 500-600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
- अन्य विकल्प: क्विनालफॉस 25 ई.सी. 2.5 मि.ली./लीटर, क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 2.5 मि.ली./लीटर, कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 50 एसपी 1 मि.ली./लीटर या फ्लूबैडिमाइड 39.35 एस.सी. 1 मि.ली./5 लीटर पानी का छिड़काव करें।
- दानेदार कीटनाशी जैसे कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी 25 कि.ग्रा./हैक्टर का प्रयोग भी कर सकते हैं।
2. तनाछेदक (स्टेम बोरर) कीट:
- क्षति: इसकी सुंडियां पौधों को नुकसान पहुँचाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में इसके प्रकोप से मुख्य तना सूख जाता है, जिसे “डेड हॉर्ट” या “व्हाइट हैड” कहते हैं। पकने की अवस्था में बालियां सूखकर सफेद दिखाई देने लगती हैं।
- नियंत्रण:
- प्रकाश प्रपंच का उपयोग करके कीट की संख्या पर निगरानी रखें।
- रोपाई के 30 दिनों बाद ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम (ट्राइकोकार्ड) 1-1.5 लाख प्रति हेक्टेयर की दर से 2-6 सप्ताह तक प्रति सप्ताह छोड़ें।
- डाइमेक्रॉन फॉस्फामिडान (85 ई.सी.) 590 मि.ली./हैक्टर या मोनोक्रोटोफॉस (36 ई.सी.) 1.5 लीटर/हैक्टर या क्लोरोपाइरीफॉस (20 ई.सी.) 2.5 लीटर/हैक्टर को 500-700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3 जी, कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 4 जी या फिप्रोनिल 0.3 जी 25 कि.ग्रा./हैक्टर का प्रयोग करें।
- अन्य विकल्प: क्विनालफॉस 25 ई.सी. 2 मि.ली./लीटर या कारटैप हाइड्रोक्लोराइड 50 एस.पी. 1 मि.ली./लीटर का छिड़काव करें।
3. ग्रास हॉपर कीट:
- क्षति: इस कीट के शिशु और वयस्क दोनों ही पत्तों को इस तरह खाते हैं जैसे उन्हें पशु चर गए हों।
- नियंत्रण:
- गर्मी में धान के खेतों की मेड़ों की खुरचाई करें, ताकि इसके अंडे नष्ट हो जाएं।
- क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 2.5 मि.ली./लीटर या क्विनालफॉस 25 ई.सी. 3 मि.ली./लीटर का छिड़काव करें।
- अन्य विकल्प: कार्बेरिल या मिथाइल पैराथियॉन पाउडर 25-30 कि.ग्रा./हैक्टर का भुरकाव करें।
4. फुदका या मधुआ हॉपर कीट:
- क्षति: फुदके तने एवं पर्णाच्छद से रस चूसकर फसल को हानि पहुँचाते हैं। इनके प्रकोप से हरी-भरी दिखने वाली फसल अचानक झुलस (hopper burn) जाती है। ये कीट तने पर होते हैं, पत्तों पर नहीं दिखते।
- नियंत्रण:
- इमिडाक्लोप्रिड 17.8 एस.एल. 1 मि.ली./3 लीटर पानी, थायोमेथोक्जम 25 डब्ल्यू पी 1 ग्राम/5 लीटर, बीपीएमसी 50 ई.सी. 1 मि.ली./लीटर, कार्बरिल 50 डब्ल्यू पी 2 ग्राम/लीटर या बुप्रोफेजिन 25 एस.सी. 1 मि.ली./लीटर पानी का छिड़काव करें।
- छिड़काव करते समय नोजल को पौधों के तनों पर रखें।
- दानेदार कीटनाशी जैसे कार्बोफ्यूरॉन 3 जी या फिप्रोनिल 0.3 जी 25 कि.ग्रा./हैक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
5. सैनिक कीट:
- क्षति: इस कीट की केवल सुंडियां ही फसल को नुकसान पहुँचाती हैं। ये नर्सरी में पौध को इस तरह कुतरकर खा जाती हैं जैसे इन्हें पशुओं ने चर लिया हो। खेत में यह कीट पत्तों की मध्य शिराओं को छोड़ते हुए पूरे पत्तों को चट कर जाते हैं।
- नियंत्रण:
- प्रकाश-प्रपंच का प्रयोग करके कीटों को एकत्र कर नष्ट कर दें।
- क्लोरोपायरीफॉस 20 ई.सी. 2.5 मि.ली./लीटर या क्विनालफॉस 25 ई.सी. 3 मि.ली./लीटर पानी का छिड़काव करें।
- अन्य विकल्प: कार्बरिल या मैलाथियॉन पाउडर 25-30 कि.ग्रा./हैक्टर का बुरकाव करें।
श्री (SRI) पद्धति से धान की खेती
श्री (System of Rice Intensification – SRI) पद्धति धान की खेती की एक उन्नत विधि है, जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक दक्षता और उपज प्रदान करती है।
श्री पद्धति की विशेषताएँ और लाभ: श्री पद्धति एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें जल उपयोग दक्षता, मृदा उत्पादकता, श्रम शक्ति एवं निवेशित पूंजी की दक्षता एक साथ बढ़ाने की क्षमता है। इस पद्धति से उगाई गई फसल द्वारा पारंपरिक विधि की अपेक्षा औसतन 10-30 प्रतिशत अतिरिक्त पैदावार विभिन्न स्थानों पर प्राप्त की गई है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित लाभों का दावा किया जाता है:
- 50 प्रतिशत तक सिंचाई जल की बचत
- 90 प्रतिशत बीज की बचत
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार
- 30-40 प्रतिशत रासायनिक उर्वरक की बचत
- लागत में कमी
रोपाई की प्रक्रिया:
- निर्धारित दूरी: रोपाई के लिए निर्धारित दूरी बनाए रखने हेतु रस्सी में बांधी गई गांठों या लकड़ी/लोहे से बने वर्गाकार मार्कर का उपयोग किया जा सकता है।
- पौध की आयु: श्री पद्धति में मात्र 8-12 दिन पुरानी पौध का उपयोग होता है।
- पौध उखाड़ने का तरीका: पौध को खुरपी से इस प्रकार उखाड़ें कि बीज चोल (seed coat) एवं जड़ों के साथ मिट्टी भी लगी रहे। यह जड़ों को कम से कम नुकसान पहुँचाता है।
- नर्सरी मैट विधि: यदि नर्सरी मैट विधि से तैयार की गई है, तो मैट को उठाकर सीधे रोपण स्थल तक ले जाया जा सकता है।
- रोपण: इसमें 2-3 पर्णीय (पत्ती वाले) पौध को 25 सें.मी.×25 सें.मी. की दूरी पर, 2-3 सें.मी. की गहराई पर अंगूठे एवं अनामिका की सहायता से, एक-एक पौध बीज चोल एवं मिट्टी सहित प्रति हिल (प्रति स्थान) बगैर पानी भरे खेत में लगाएं (या बहुत कम पानी में)।
- शीघ्र रोपाई: पौध की जड़ों को सूखने से बचाने के लिए नर्सरी से निकालने के आधे घंटे के भीतर रोपाई कर लेनी चाहिए।
खरपतवार नियंत्रण (कोनो वीडर द्वारा):
- लाभ: कोनो वीडर द्वारा खरपतवार नियंत्रण करने से खरपतवार मिट्टी में दबकर सड़ते हैं, जिससे जैविक खाद बनती है और पौधों को पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
- मृदा पर प्रभाव: इसके उपयोग से मिट्टी भुरभुरी होती है और वायु संचार बढ़ जाता है, जिससे पौधों की वृद्धि बेहतर होती है।
- वीडर चलाने का समय: रोपाई के 10 दिनों बाद से प्रत्येक 10 दिनों के अंतराल पर 3-4 बार वीडर चलाना चाहिए।
- नमी की आवश्यकता: इसके लिए खेत में पर्याप्त नमी का होना आवश्यक है।
श्री पद्धति धान की खेती को अधिक टिकाऊ और आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने में सहायक है।
धान की संडा रोपाई (Wet Transplanting / Sanda Ropai)
संडा रोपाई, जिसे कुछ क्षेत्रों में “वेट ट्रांसप्लांटिंग” भी कहा जाता है, धान की खेती की एक विशेष विधि है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार जैसे क्षेत्रों की विशिष्ट पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करने के लिए विकसित की गई है।
समस्या: पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार में धान की फसल को जुलाई के प्रारंभ से अक्टूबर के मध्य तक लगभग 100 दिनों तक अत्यधिक नम अवस्था का सामना करना पड़ता है।
- इन क्षेत्रों में धान की खेती अप्लैंड (ऊँचे) या लो लैंड (नीचे) खेतों में की जाती है।
- अप्लैंड खेतों में: मानसून आने के बाद लंबे ब्रेक (कम बारिश) की स्थिति में धान की फसल को जल की कमी का सामना करना पड़ता है।
- लो लैंड खेतों में: बहुत अधिक वर्षा हो जाने पर खेतों में आवश्यकता से अधिक पानी, जल निकास की व्यवस्था समुचित न होने से इकट्ठा हो जाता है, जिससे रोपाई में विलंब हो जाता है।
- इन दोनों ही स्थितियों में धान के पौधों में कम कल्ले निकलते हैं तथा बढ़वार अच्छी नहीं होती है, जिससे उपज प्रभावित होती है।
संडा विधि का समाधान: ऐसे में संडा विधि अपनाई जाती है, जिसमें पूर्व में रोपे गए मदर प्लांट (मूल पौधे) से कल्लों (टिलर्स) को अलग करके प्राप्त किया जाता है और रोपाई दोबारा की जाती है। यह विधि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वस्थ पौध सामग्री और बेहतर कल्ले निकलने को सुनिश्चित करती है।
संडा रोपाई की प्रक्रिया:
- पहली रोपाई:
- 3 सप्ताह की अवधि के पौधे तैयार करें।
- इन पौधों की रोपाई 20 सें.मी.×10 सें.मी. की दूरी पर करें। यह पहली नर्सरी या प्रारंभिक रोपण होता है।
- दूसरी रोपाई (संडा रोपाई):
- पहली रोपाई के 3 सप्ताह बाद, पहली बार रोपे गए धान के पौधों से विकसित स्वस्थ कल्लों को अलग किया जाता है।
- इन कल्लों को 10 सें.मी.×10 सें.मी. की घनी दूरी पर दोबारा रोपना चाहिए।
यह विधि सुनिश्चित करती है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में भी धान के पौधों को पर्याप्त पोषण और स्थान मिले, जिससे उनकी बढ़वार और कल्ले निकलने की क्षमता में सुधार हो।
धन्यवाद