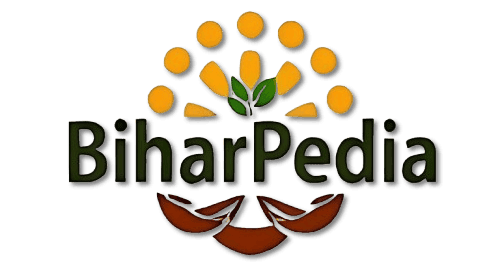जुलाई (आषाढ़-श्रावण) माह के प्रमुख कृषि कार्य (Agricultural work in July Month):
जुलाई माह खरीफ की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां खेती वर्षा पर निर्भर करती है। इस महीने मानसून आ चुका होता है, इसलिए सभी कार्यों को समय से किया जाना अत्यंत आवश्यक है। खरीफ फसलों का देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में आधे से भी अधिक का योगदान होता है। खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे- धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, कुसुम, तिल, कपास एवं जूट आदि प्रमुख हैं। फसलों के उत्पादन में उपयुक्त सस्य विधियां अपनाकर उत्पादन लागत में कमी एवं प्रति इकाई उपज में वृद्धि की जा सकती है। अनुसंधानों से ज्ञात हुआ है कि अधिक उपज देने वाली उन्नत प्रजातियों की गुणवत्ता का स्वस्थ बीज, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, समुचित जल प्रबंधन, एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन, उपयुक्त समय पर फसल की कटाई एवं मड़ाई तथा उपयुक्त भंडारण इत्यादि अपनाकर किसान लागत कम करके उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकते हैं। कुल मिलाकर, जुलाई का महीना कृषि गतिविधियों के लिए अत्यंत व्यस्त और निर्णायक होता है, जो पूरे कृषि चक्र की नींव रखता है।
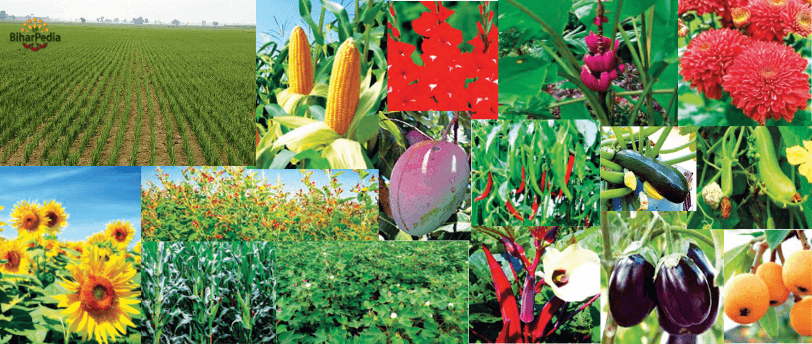
फसल उत्पादन (Crop Production):
धान की नर्सरी (Paddy Nursery):
- जलवायु: समशीतोष्ण जलवायु में 20–35°C तापमान और अच्छी वर्षा जरूरी है।
- मृदा: मटियार, मटियार दोमट या चिकनी मिट्टी जिसमें जलधारण क्षमता अधिक हो। pH 6.5–8.5 उपयुक्त।
- खेत की तैयारी: गर्मी में गहरी जुताई, फिर 2–3 बार जुताई, समतलीकरण और मेड़बंदी करें।
- रोग नियंत्रण: 20–25 किलो ट्राइकोडर्मा + 60 किलो सड़ी गोबर की खाद मिलाकर खेत में डालें।
- रोपाई: 20–25 दिन पुरानी 4–5 पत्तों वाली पौध लगाएं। मध्यम व देर वाली किस्में – जुलाई के पहले पखवाड़े तक। जल्दी पकने वाली – जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक। सुगंधित किस्म – जुलाई के अंत में रोपें। दूरी: 20–30×15 से.मी. और 2–3 पौधे प्रति स्थान। ऊसर भूमि में: 35–40 दिन पुरानी पौध, दूरी 15×10 से.मी. और 3–4 पौधे लगाएं।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- धान की बौनी प्रजातियों के लिए (प्रति हेक्टेयर): नाइट्रोजन: 100–120 कि.ग्रा., फॉस्फोरस: 60 कि.ग्रा., पोटाश: 60 कि.ग्रा., जिंक सल्फेट: 25 कि.ग्रा.।
- बासमती प्रजातियों के लिए: नाइट्रोजन: 80–100 कि.ग्रा., फॉस्फोरस: 50–60 कि.ग्रा., पोटाश: 40–50 कि.ग्रा., जिंक सल्फेट: 20–25 कि.ग्रा.
- खाद देने का समय:
- फॉस्फोरस, पोटाश व जिंक → अंतिम जुताई के समय
- यूरिया (तीन भागों में): रोपाई के 5–8 दिन बाद→25–30 दिन बाद (कल्ले फूटने पर)→50–60 दिन बाद (फूल आने से पहले)
- हरी खाद या गोबर खाद हो तो नाइट्रोजन की मात्रा 20–25 कि.ग्रा./हेक्टेयर तक कम करें।
- जैव उर्वरक (नील हरित शैवाल): 10–15 कि.ग्रा./हेक्टेयर रोपाई के एक सप्ताह बाद खड़े पानी में छिड़काव करें। हर साल 3 वर्षों तक प्रयोग करें। खेत में पानी बना रहे, सूखने न दें।
- खरपतवार नियंत्रण: खरपतवार नमी, पोषक तत्व और धूप के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं।
- हानि: रोपाई वाले धान में: 15–40% और सीधे बोये गये धान में: 30–85%
- खरपतवार पोषक तत्वों का अत्यधिक शोषण कर लेते हैं जिससे फसल कमजोर हो जाती है।
- श्री पद्धति: यह धान की खेती की एक उन्नत तकनीक है जिससे 10–30% तक अधिक उपज मिलती है, 50% तक पानी की बचत होती है, 90% तक बीज की बचत, 30–40% तक रासायनिक खाद की बचत और मृदा स्वास्थ्य में सुधार और लागत में कमी आती हैं।
- मुख्य विशेषताएँ: 8–12 दिन पुरानी पौध से रोपाई की जाती है। 25×25 से.मी. दूरी पर एक-एक पौधा लगाया जाता है। रोपाई बिना पानी भरे खेत में, अंगूठा और अनामिका की सहायता से करें। बीज चोल व मिट्टी सहित पौध लगानी चाहिए। पौध उखाड़ने के आधे घंटे में रोपाई करें, ताकि जड़ सूखे नहीं।
- खरपतवार नियंत्रण: कोनो वीडर का प्रयोग करें। हर 10 दिन पर 3–4 बार वीडर चलाएं। खरपतवार मिट्टी में दबकर जैविक खाद बनते हैं। इससे मिट्टी भुरभुरी होती है, व वायु संचार बढ़ता है।
- श्री पद्धति अपनाकर किसान कम संसाधन में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल और आर्थिक रूप से लाभकारी तकनीक है।
- संडा रोपाई: यह एक विशेष तकनीक है जिसमें धान की दो बार रोपाई की जाती है। दूसरी रोपाई के लिए पहली बार लगाए गए पौधों से निकले कल्लों (संडा) को पुनः रोपा जाता है।
- पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं पश्चिमी बिहार जैसे क्षेत्रों में जहां जुलाई से अक्टूबर तक खेतों में अधिक या अत्यधिक नमी रहती है। लो लैण्ड में जलभराव और अपलैण्ड में पानी की कमी की स्थिति में इस विधि का उपयोग किया जाता है।
- फायदे: पौधों में अधिक कल्ले निकलते हैं, पौधे की बढ़वार बेहतर होती है, खाली जगहों की भरपाई हो जाती है और उत्पादन में इजाफा होता है।
- रोपाई की विधि:
- पहली रोपाई– 3 सप्ताह पुरानी पौध और दूरी: 20×10 से.मी. है।
- दूसरी रोपाई (संडा रोपाई)– पहली रोपाई के 3 सप्ताह बाद, पहली फसल से निकले कल्लों (संडा) से और दूरी: 10×10 से.मी. है।
- संडा रोपाई तकनीक से धान की फसल को जलभराव और जल की कमी जैसी विषम परिस्थितियों में भी बेहतर उत्पादन मिल सकता है। यह खाली स्थानों की भरपाई और पौधों की संख्या बढ़ाने में मदद करता है।
धान की वैज्ञानिक खेती की विस्तृत जानकारी
धान की सीधी बुआई (Direct Seeding of Rice – DSR):
- धान की सीड ड्रिल (सीधी बुआई) एक संसाधन संरक्षित खेती तकनीक है, जिससे 20% पानी, समय और श्रम की बचत होती है। यह विधि पारंपरिक रोपाई की तुलना में 10-15 दिन पहले फसल तैयार कर देती है, जिससे अगली फसल की समय पर बुआई संभव होती है।
- प्रमुख मशीनें: जीरो टिल प्लान्टर, टर्बो सीडर, पीसीआर प्लान्टर, रोटरी डिस्क ड्रिल, डब्ल्यू डिस्क कल्टीवेटर
- फायदे: पानी, समय और श्रम की बचत, फसल जल्दी तैयार, अगली फसल की समय पर बुआई और संपूर्ण प्रणाली की उत्पादकता में वृद्धि।
- बुआई के समय ध्यान देने योग्य बातें: बुआई से पहले खरपतवारनाशी जैसे ग्लाइफोसेट या पैराक्वाट का प्रयोग करें। बीज दर: 20–25 कि.ग्रा./हेक्टेयर। DAP: 120 कि.ग्रा./हेक्टेयर। बीज गहराई: 3–4 से.मी. (अधिक गहराई से अंकुरण कम होगा)। ड्रिल की नली बंद न हो, यह सुनिश्चित करें। यूरिया व म्यूरेट ऑफ पोटाश टॉप ड्रेसिंग के रूप में ही डालें, खाद बक्से में नहीं।
- नवीन किस्में (रोबिनोवीड बासमती): पूसा बासमती 1985 और पूसा बासमती 19791 (भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली द्वारा विकषित)
- सीड ड्रिल द्वारा सीधी बुआई, कम लागत में अधिक उत्पादन पाने की वैज्ञानिक और आधुनिक तकनीक है, जो खेती को टिकाऊ व लाभकारी बनाती है।
धान की सीधी बुआई (Direct Seeding of Rice – DSR) तकनीक की पूरी जानकारी।
मक्का (Maize):
- बुआई का समय:
- सिंचित क्षेत्रों में: सिंचित क्षेत्रों में मक्का की बुआई मानसून आने के 10-15 दिनों पहले कर देनी चाहिए, ताकि मानसून की पहली बारिश का लाभ मिल सके।
- वर्षा आधारित क्षेत्रों में: वर्षा आधारित क्षेत्रों में सामान्यतः वर्षा के आगमन पर ही मक्का की बुआई की जाती है।
- अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में: ऐसे क्षेत्रों में मेड़ (ridges) बनाकर उनके ऊपर मक्का की बुआई करनी चाहिए, ताकि जल जमाव से बचा जा सके।
- कम वर्षा वाले क्षेत्रों में: कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कूड़ (furrows) में बुआई करनी चाहिए, ताकि नमी का बेहतर संरक्षण हो सके।
- बीज दर:
- संकर प्रजातियों: 20-22 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
- संकुल प्रजातियों: 18-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
- देशी-छोटे दाने वाली प्रजाति: 16-18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
- स्वीटकॉर्न (Sweetcorn): स्वीटकॉर्न का बीज हल्का होने के कारण 7-10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त रहता है।
- बीजोपचार और अंकुरण:
- अच्छे अंकुरण के लिए बीजों को रातभर पानी में भिगोकर तथा सुबह छाया में सुखाकर बोना चाहिए।
- बीज बोने से पूर्व 1 किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2.0 ग्राम कार्बण्डाजिम से शोधित कर लें। यह बीज जनित रोगों से बचाव में मदद करता है।
- जैव उर्वरक: बुआई से पहले एजोस्पिरिलम (Azospirillum) के 3-4 पैकेट से उपचार करने से विशेष रूप से बेबीकॉर्न की गुणवत्ता और उपज में वृद्धि होती है।
- बुआई की दूरी:
- सामान्य मक्का: पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी क्रमशः 75 सें.मी.×20 सें.मी. या 60 सें.मी.×25 सें.मी. रखते हैं।
- विशेष मक्का (विभिन्न उपयोगों के लिए):
- स्वीटकॉर्न: 60−75 सें.मी.×20−25 सें.मी.
- बेबीकॉर्न: 45 सें.मी.×15 सें.मी.
- पॉपकॉर्न: 60 सें.मी.×20 सें.मी.
- दीमक नियंत्रण: जिन क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप होता है, वहां आखिरी जुताई पर क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई.सी. की 2.5 लीटर मात्रा को 5.0 लीटर पानी में घोलकर 20 किलोग्राम बालू में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से मिट्टी में मिला देना चाहिए।
मक्का की खेती में अधिकतम उपज और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए सही किस्म का चयन, संतुलित पोषण और प्रभावी खरपतवार प्रबंधन महत्वपूर्ण हैं।
- मक्का की उन्नत प्रजातियाँ:
- उन्नत संकर प्रजातियाँ (Improved Hybrid Varieties): उन्नत पूसा एचएम-4, पूसा जवाहर संकर मक्का 1, एचएम-4, एएच-4725, एसएमएच-3904, जेकेएमएच-502 आदि।
- प्रोटीनयुक्त प्रजातियाँ (Protein-rich Varieties): उन्नत पूसा विवेक क्यूपीएम-9 (QPM-9), एचक्यूपीएम-1, 4, 5, 7 (HQPM-1, 4, 5, 7) आदि प्रमुख हैं। इन प्रजातियों को उन क्षेत्रों में बोना चाहिए जहां सिंचाई देकर समय से बुआई हो सके।
- स्वीटकॉर्न की उन्नत प्रजातियाँ (Improved Sweetcorn Varieties): एचएम-4, गंगा सफेद-2, पूसा अर्ली हाइब्रिड मक्का-3 आदि प्रमुख हैं।
- बेबीकॉर्न (शिशु मक्का) की उन्नत प्रजातियाँ (Improved Babycorn Varieties): भुट्टे की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए बेबीकॉर्न की प्रजाति का चयन करें। ऐसी प्रजातियाँ जो भुट्टे के दानों का आकार और दानों का सीधी पंक्ति में होना, एक समान भुट्टे पकने वाली हों, और जो मध्यम ऊंचाई की अगेती परिपक्व (55 दिन) हों, उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। बेबीकॉर्न की उन्नत प्रजातियाँ जैसे- शुगर बेबी, वीएल-78, एचएम-4, वीएन-42, एचएएम-129, गोल्डन बेबी एवं जी 5414 आदि प्रमुख हैं।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- मृदा परीक्षण के आधार पर: उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर ही करना चाहिए।
- नाइट्रोजन (N) की मात्रा: दीर्घकालिक प्रजातियों के लिए: 120-150 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर। मध्यम पकने वाली प्रजातियों के लिए: 80-100 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर। जल्दी पकने वाली प्रजातियों के लिए: 60-80 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर।
- फॉस्फोरस (P) और पोटेशियम (K): सभी प्रजातियों के लिए 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 50 कि.ग्रा. पोटेशियम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होती है।
- स्वीटकॉर्न के लिए विशिष्ट: नाइट्रोजन: 120 कि.ग्रा., फॉस्फोरस: 60 कि.ग्रा., पोटेशियम: 40 कि.ग्रा. ,जिंक सल्फेट: 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।
- बेबीकॉर्न में उर्वरक का प्रयोग:
- बेसल ड्रेसिंग (बुवाई के समय): 75:60:20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से NPK (नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम)।
- शीर्ष ड्रेसिंग (बुवाई के तीन सप्ताह बाद): 80 कि.ग्रा. नाइट्रोजन और 20 कि.ग्रा. पोटाश।
- जिंक सल्फेट का प्रयोग: यदि मक्का की बुआई बलुई मृदा में की जाती है या खेत में जिंक की कमी हो तो 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट को खेत में बुवाई से पूर्व डालना चाहिए।
- प्रयोग विधि: नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फॉस्फोरस, पोटेशियम एवं जिंक सल्फेट की पूरी मात्रा बुवाई के समय 10-15 सें.मी. की गहराई पर पंक्तियों में दें। शेष नाइट्रोजन बाद में दें।
- खरपतवार नियंत्रण:
- निराई का समय: मक्का में पहली निराई अंकुरण के 15 दिनों बाद तथा दूसरी निराई 35-40 दिनों बाद करनी चाहिए।
- शाकनाशी का प्रयोग:
- एट्राजीन (Atrazine): माध्यम से भारी मृदा में: 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर। हल्की मृदा में: 1.25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर। इसे बुवाई के अगले 2 दिनों में 500 लीटर प्रति हेक्टेयर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यह शाकनाशी एकवर्षीय घासकुल एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को बहुत ही प्रभावी रूप से नियंत्रित करता है।
- मजबूत खरपतवारों का नियंत्रण: मजबूत खरपतवारों जैसे कि वन पट्टा, रसभरी को नियंत्रित करने हेतु बुवाई के दो दिनों के अंदर एट्राटॉफ 600 ग्राम प्रति एकड़, स्टाम्प 30 ई.सी. या ट्रेफ्लान 48 ई.सी. (ट्रेफ्लुरेलिन) प्रत्येक 1 लीटर प्रति एकड़ अच्छी तरह से मिलाकर 200 लीटर पानी के साथ प्रयोग करने पर अच्छे परिणाम आते हैं।
बाजरा (Pearl Millet)
- बाजरा एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जहाँ पानी की उपलब्धता सीमित होती है।
- बुआई:
- समय: बाजरे की बुआई जुलाई के द्वितीय पखवाड़े में करनी चाहिए।
- बीज दर: एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 4-5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
- उपयुक्त क्षेत्र और मृदा: बाजरे की फसल भारी वर्षा वाले उन क्षेत्रों में अच्छी तरह से ली जा सकती है, जहां पर पानी का भराव न हो। इसके लिए बलुई दोमट मृदा अत्यंत उपयुक्त होती है।
- देरी से बुआई की स्थिति में रोपण: यदि किसी कारण से बाजरे की बुआई समय पर नहीं की जा सकी हो, तो फसल देरी से बोने की अपेक्षा उसे रोपना अधिक लाभप्रद होता है।
- एक हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे रोपने के लिए लगभग 500-600 वर्ग मीटर में 2-2.5 किलोग्राम बीज की जुलाई में बुआई कर देनी चाहिए।
- लगभग 2-3 सप्ताह की पौध रोपनी चाहिए।
- जब पौधों को क्यारियों से उखाड़ें, तो क्यारियों में नमी बनाए रखना आवश्यक है, ताकि जड़ों को क्षति न पहुंचे।
- रोपण दूरी: पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी 45−50 सें.मी.×10−15 सें.मी. रखते हुए एक छेद में केवल एक ही पौधे की रोपाई करें।
- बाजरे की उन्नत प्रजातियाँ:
- उन्नत संकर प्रजातियाँ: पूसा-23, पूसा 415, पूसा-605, एचएचबी-50, एचएचबी-67 और एचएचडी-68।
- बाजरे की संकुल किस्में (Composite Varieties): पूसा-443, पूसा कम्पोजिट-643, पूसा कम्पोजिट-612, राज बाजरा चारी-2, राज-171, आईसीएमवी-155 (ICMV-155), डब्ल्यूसीसी-75 (WCC-75), एचसी-4 (HC-4), एचसी-10 (HC-10) और आईसीटीपी-8203 (ICTP-8203) प्रमुख हैं।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- देशी प्रजातियों के लिए: 20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 25 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 25 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करें।
- संकर प्रजातियों के लिए: 80 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर बुआई के समय प्रयोग करें।
- प्रयोग विधि: सभी परिस्थितियों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा लगभग 3-4 सें.मी. की गहराई पर डालनी चाहिए।
- नाइट्रोजन का शेष भाग: नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा अंकुरण से 4-5 सप्ताह बाद खेत में छिड़ककर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देनी चाहिए।
ज्वार (Sorghum)
- ज्वार एक महत्वपूर्ण खरीफ फसल है, जिसकी खेती विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों में की जाती है।
- बुआई:
- समय: ज्वार की बुआई इस माह (जुलाई) के प्रथम पखवाड़े तक पूरी कर लेनी चाहिए।
- बीजोपचार: बुआई से पूर्व बीज को कार्बण्डाजिम (Carbendazim) या एग्रोसन जीएन (Agrosan GN) अथवा कैप्टॉन (Captan) आदि से 2-5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित कर लेना चाहिए। यह बीज जनित रोगों से बचाव में सहायक है।
- जैव उर्वरक: इसके अतिरिक्त, बीज को जैव उर्वरक एजोस्पीरीलम (Azospirillum) एवं पीएसबी (PSB) से भी उपचारित करने से 15-20 प्रतिशत अधिक उत्पादन लिया जा सकता है।
- बीज दर: ज्वार की बुआई के लिए 12-15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
- बुआई की दूरी: इसके लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी एवं पौधे से पौधे की दूरी 45 सें.मी.×15 सें.मी. रखी जानी आवश्यक है।
- किस्मों का चयन: ज्वार की उन्नत संकर प्रजातियां जैसे- सीएसएच-1 (CSH-1), सीएसएच-9 (CSH-9), सीएसएच-11 (CSH-11), सीएसएच-13 (CSH-13) आदि प्रमुख हैं।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- सिंचित क्षेत्रों में: ज्वार की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए सिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 100-120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50-60 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 40-50 किलोग्राम पोटाश की आवश्यकता पड़ती है।
- असिंचित क्षेत्रों में: असिंचित क्षेत्रों में प्रति हेक्टेयर 50-60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30-40 किलोग्राम फॉस्फोरस तथा 30-40 किलोग्राम पोटाश पर्याप्त होता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्व: जिंक तथा आयरन ज्वार के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। इन तत्वों की कमी पूरा करने के लिए जिंक का 0.2 प्रतिशत तथा आयरन का 0.15 प्रतिशत घोल का पर्णीय छिड़काव बुआई के 35-40 दिनों बाद अवश्य कर देना चाहिए।
- खरपतवार प्रबंधन:
- निराई-गुड़ाई: ज्वार की खेती में निराई-गुड़ाई का अधिक महत्व है।
- खरपतवारनाशी का प्रयोग: साथ ही, निम्नलिखित खरपतवारनाशियों में से किसी एक का प्रयोग बुआई के तुरंत बाद अंकुरण के पूर्व करने से खरपतवार नष्ट हो जाते हैं:
- एट्राजीन (Atrazine) (50% डब्ल्यू.सी.) 0.75-1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
- एलाक्लोर (Alachlor) (50 ई.सी) 1.5-2.0 लीटर प्रति हेक्टेयर
- एट्राजीन + पेण्डीमेथिलीन (Pendimethalin) 0.75-1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
- एट्राजीन + एलाक्लोर 0.75-1.0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर
- इन घुलनशील चूर्णों या तरल सांद्रणों को 600-800 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग करना चाहिए।
मूंगफली (Peanuts)
- मूंगफली (Groundnut) भारत की एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जिसकी खेती देश के कई हिस्सों में की जाती है।
- जलवायु एवं मृदा:
- जलवायु: मूंगफली की खेती उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले प्रदेशों में की जाती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए 60 से 130 सें.मी. वर्षा काफी होती है।
- मृदा: इसकी खेती के लिए उचित जल निकासी वाली हल्की पीली दोमट मृदा सबसे उपयुक्त होती है। साथ ही भूमि का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए।
- उन्नत प्रजातियाँ: जीजी 3, जीजी 20, जे 11, जीएयूजी 1, जेएल 24, टीएजी 24, टीएजी 26, और आरजी-141 आदि।
- बुआई:
- समय: खरीफ मौसम की फसल की बुआई का उचित समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। हालांकि, असिंचित क्षेत्रों में जहां बुआई मानसून के बाद की जाती है, जुलाई के पहले पखवाड़े में बुआई के काम को पूरा कर लें, ताकि निक्रोसिस रोग से बचा जा सके।
- बीज दर: मूंगफली की मध्यम और अधिक फैलने वाली किस्मों में क्रमशः 80-100 और 60-80 कि.ग्रा. बीज प्रति हेक्टेयर। गुच्छेदार किस्मों में बीज की उचित मात्रा 100-125 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।
- बुआई की दूरी और गहराई: गुच्छेदार किस्मों को 30 सें.मी.×10 सें.मी.।फैलने वाली किस्मों को 45−60 सें.मी.×10−15 सें.मी. की दूरी एवं 4-6 सें.मी. की गहराई पर बोएं।
- मेड़ों पर बुआई: यदि संभव हो तो मूंगफली की बुआई मेड़ों पर करें।
- बीजोपचार: बुआई से पूर्व बीज को 2-3 ग्राम थीरम या कार्बेण्डाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें।
- राइजोबियम कल्चर: इस उपचार के 5-6 घंटे बाद, बीज को उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। उपचार के बाद बीज को छाया में सुखाएं एवं शीघ्र ही बुआई के लिए उपयोग करें।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- कार्बनिक खाद: मृदा परीक्षण के अभाव में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के साथ-साथ 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद का उपयोग करें।
- रासायनिक उर्वरक (सिंचित क्षेत्रों में): नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्रिया के शुरू होने से पहले की मांग की पूर्ति के लिए सिंचित क्षेत्रों में 20-30 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40-60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 30-40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
- रासायनिक उर्वरक (बारानी क्षेत्रों में): बारानी क्षेत्रों में 15-20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 30-40 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 20-25 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
- गंधक और कैल्शियम: इनके अतिरिक्त गंधक और कैल्शियम का मूंगफली की उपज और गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा गया है, जिसके लिए 200-400 कि.ग्रा. जिप्सम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
- उर्वरक प्रयोग का समय:
- नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और जिप्सम की आधी मात्रा बुआई के समय मृदा में अच्छी तरह मिला दें।
- जिप्सम की शेष आधी मात्रा को फूल निकलने के समय 5 सें.मी. की गहराई पर पौधे के पास दिया जाना चाहिए।
- सूक्ष्म पोषक तत्व:
- जस्ते की कमी की पूर्ति हेतु 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
- बोरॉन की कमी की पूर्ति हेतु 2 कि.ग्रा. बोरेक्स प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें।
- खरपतवार प्रबंधन:
- खरपतवार का सही नियंत्रण न करने पर फसल उत्पादन में 30-50 प्रतिशत तक कमी आ जाती है।
- निराई-गुड़ाई: इसके लिए कम से कम दो बार निराई-गुड़ाई, 20-25 दिनों और 40-45 दिनों पर की जानी चाहिए।
- रासायनिक खरपतवार नियंत्रण:
- एलाक्लोर (50 प्रतिशत ई.सी.) 1.5-2.0 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर
- या पेण्डीमेथिलीन (30 प्रतिशत ई.सी.) 1 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर
- इन खरपतवारनाशियों का बुआई के बाद दूसरे दिन 700-800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- फसल की बुआई के पूर्व फ्लूक्लोरेलिन 1 कि.ग्रा. सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करके मिट्टी में मिलाने से भी खरपतवारों को नियंत्रित किया जा सकता है।
गन्ना (Sugarcane)
- यूरिया का प्रयोग: फसल में शेष बची एक बोरी यूरिया जुलाई में मानसून वर्षा आने पर डालें।
- मिट्टी चढ़ाना: गन्ने की देर से बोई गई फसल में निराई-गुड़ाई करने के बाद इस माह मिट्टी चढ़ाने का कार्य पूरा कर लें। यह पौधों को सहारा देने और खरपतवार नियंत्रण में मदद करता है।
- जल निकास: जल निकास का उचित प्रबंधन करें। अधिक वर्षा की स्थिति में खेतों से अतिरिक्त पानी निकालना आवश्यक होता है।
- सिंचाई: पर्याप्त वर्षा न होने पर 15-20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करते रहें।
- बंधाई: शरद कालीन गन्ने को गिरने से बचाने के लिए बंधाई अवश्य करें।
- पौध संरक्षण:
- चोटीबेधक (Top Borer): चोटीबेधक की मादा तितली जुलाई माह में पत्तियों की निचली सतह पर समूह में अंडे देती है। अंडे वाली पत्तियों को नष्ट कर दें। कार्बोफ्यूरॉन 3 जी 25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य प्रयोग करें। चोटीबेधक के नियंत्रण हेतु 4 ट्राइकोकार्ड प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
- गुरदासपुर बेधक (Gurdaspur Borer): गुरदासपुर बेधक के नियंत्रण हेतु सूखे अगोले को काटकर जमीन में दबा दें। क्लोरोपाइरीफॉस 20 ई.सी. 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें।
- सफेद गिडार (White Grub): सफेद गिडार के नियंत्रण हेतु लाइट ट्रैप का उपयोग करें या कीटनाशी छिड़काव कर नियंत्रण करें।
सूरजमुखी (Sunflower)
- सूरजमुखी (Sunflower) एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जिसकी खेती तेल उत्पादन के लिए की जाती है।
- जलवायु: सूरजमुखी की 26 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छी फसल ली जा सकती है। पौधे के अच्छे विकास के लिए सूर्य के प्रकाश और गर्मी की आवश्यकता होती है।
- मृदा: इसकी खेती अच्छे जल निकास वाली सभी तरह की मृदा में की जा सकती है। दोमट एवं बलुई दोमट मृदा जिसका पी-एच मान 6.5-8.5 हो, इसके लिए बेहतर होती है।
- सूरजमुखी की उन्नत प्रजातियाँ:
- संकर प्रजातियाँ: केवीएसएसएच 1, एसएच-3322, एमएसएफएच-1785-90, केवीएसएसएच-44, डीआरएसएच-1, पीएसएफएच-118, पीएसएफएच-569, एचएसएफएच-848, मारूती, केवीएसएसएच-41।
- उन्नत संकुल प्रजातियाँ: सूर्या, माडर्न, डीआरएस-108, को-5, टीएएसएफ-82, एलएसएफ-8, फुले रविराज आदि प्रमुख हैं।
- बुआई:
- समय: सूरजमुखी की बुआई इस माह (जुलाई) के प्रथम पखवाड़े में कर लें।
- बीजोपचार: बुआई से पूर्व बीजों को थीरम या कैप्टॉन की 3.0 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करें। इससे मृदाजनित रोगों से बीज सड़ता नहीं है और जमाव अच्छा होता है।
- बीज दर और दूरी:
- संकर प्रजातियों: 7-8 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर को 60 सें.मी.×20 सें.मी. की दूरी पर।
- संकुल प्रजातियों: 12-15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर को 45 सें.मी.×20 सें.मी. की दूरी पर करनी चाहिए।
- बुआई विधि: बुआई सीडड्रिल या पंक्तियों में करें।
- विरलन (Thinning): जब पौधे लगभग 10 दिनों के हो जाएं और कहीं पर एक से अधिक पौधे दिखाई पड़ें, तो ओज वाले पौधे को छोड़कर बाकी को उखाड़ दें।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- मृदा परीक्षण के आधार पर: सामान्यतः सूरजमुखी की फसल में उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना चाहिए।
- सामान्य अनुशंसा (मृदा परीक्षण न होने पर): मृदा परीक्षण न होने की दशा में 40 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 40 कि.ग्रा. पोटाश एवं 25 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए।
- खरपतवार नियंत्रण:
- रासायनिक खरपतवार नियंत्रण: रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेण्डीमेथिलीन (30 ई.सी.) 3.3 लीटर या प्री-इमरजेंस फ्लूक्लोरीन का 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 1-2 दिनों बाद छिड़क देना चाहिए।
- गुड़ाई: यदि आवश्यकता पड़े तो 30-35 दिनों बाद एक गुड़ाई करें। इस समय पौधों के दोनों तरफ मिट्टी भी चढ़ा देनी चाहिए।
तिल (Sesame)
- तिल एक महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, जिसकी खेती उसके तेल युक्त बीजों के लिए की जाती है।
- भूमि का चयन एवं तैयारी:
- मृदा: तिल की खेती मटियार एवं चिकनी दोमट मृदा में सफलतापूर्वक की जा सकती है।
- खेत की तैयारी: रबी-जायद की फसलें काटने के बाद दो जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद कल्टीवेटर या देसी हल से दो बार जुताई करके खेत अच्छी तरह समतल कर लेना चाहिए।
- उन्नत किस्में: गुजरात तिल नं-1, गुजरात तिल नं-2, फुले तिल नं-1, प्रताप, ताप्ती, पदमा, एन.-8, डी.एम.-1 आदि।
- बुआई:
- समय: खरीफ फसल के लिए जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक तिल की बुआई को उपयुक्त पाया गया है।
- बीज दर (प्रति हेक्टेयर):समय से बुआई के लिए: 3-4 कि.ग्रा., देर से बुआई के लिए: 4-5 कि.ग्रा.
- बीज शोधन: बीजजनित रोगों से बचाव हेतु 2.5 ग्राम थीरम या कैप्टॉन प्रति किलोग्राम की दर से बीज शोधन हेतु प्रयोग करें।
- बुआई की दूरी और गहराई: पंक्तियों के बीच का फासला 30-45 सें.मी. का रखें। बीज को 1.5-2.5 सें.मी. की गहराई पर डालें।
- छंटाई/विरलन: बुआई के 15 से 20 दिनों बाद पौधों की छंटाई करते समय पौधे से पौधे की दूरी 10-15 सें.मी. रखें।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- उर्वरकों की मात्रा मृदा की जांच और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है।
- मृदा जांच संभव न होने की अवस्था में:
- सिंचित क्षेत्रों में: 40-50 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 20-30 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 20 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर।
- वर्षा आधारित फसल में: 20-25 कि.ग्रा. नाइट्रोजन और 15 से 20 कि.ग्रा. फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर।
- गंधक का उपयोग: मुख्य तत्वों के अतिरिक्त 10 से 20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर गंधक का उपयोग करने से तिल की उपज में वृद्धि की जा सकती है।
- उर्वरक प्रयोग का समय:
- सिंचित क्षेत्रों में: नाइट्रोजन की आधी मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय बीज से 3-4 सें.मी. गहराई पर प्रयोग करें।
- असिंचित क्षेत्रों में: सभी उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय बीज से 3-4 सें.मी. गहराई पर प्रयोग करें।
- शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को बुआई के 30-35 दिनों बाद खड़ी फसल में प्रयोग करें (टॉप ड्रेसिंग)।
- खरपतवार नियंत्रण: खेत को बुआई के 25-30 दिनों तक खरपतवारों से मुक्त रखना अनिवार्य है।
- निराई-गुड़ाई: पहली निराई-गुड़ाई फसल बोने के 15 से 20 दिनों के अंदर करनी चाहिए। यदि खरपतवार अधिक हो, तो बुआई के 35 से 40 दिनों के अंदर दूसरी निराई-गुड़ाई करें।
- रासायनिक नियंत्रण:
- तिल में 1 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से फ्लूक्लोरेलिन सक्रिय दवा को 400-500 लीटर पानी में घोलकर गुड़ाई से पहले खेत में छिड़कने से भी खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। फसल बोने से पहले दवाई को सतही मिट्टी में मिला दें।
- इसके अतिरिक्त एलाक्लोर (1.75 कि.ग्रा.) या पेण्डीमेथिलीन (1 कि.ग्रा.) का प्रयोग बुआई के 2-3 दिनों के अंदर करें (प्री-इमरजेंस)।
अरहर, मूंग एवं उड़द(Pigeon Pea, Moong and Urad)
- अरहर (Redgram/Pigeonpea), मूंग (Greengram) और उड़द (Blackgram) भारत की महत्वपूर्ण दलहनी फसलें हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि करने में सहायक हैं।
- बुआई का समय:
- अरहर: अगेती एवं पछेती फसल के रूप में खेती की जाती है। सिंचित क्षेत्रों में अगेती अरहर की बुआई मध्य जून में पलेवा करके अवश्य करें।
- मूंग: मूंग की फसल को मध्य जुलाई से अगस्त के दूसरे सप्ताह तक बोना चाहिए।
- उड़द: उड़द की बुआई का उचित समय जुलाई के प्रथम पखवाड़े तक अच्छा माना जाता है। देर से बुआई करने पर उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- मृदा का चयन: हालाँकि, अरहर, मूंग एवं उड़द को अधिकांश मृदा में उगाया जा सकता है। फिर भी, मृदा का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि खेत ऊंचा एवं समतल हो तथा उसमें जल निकास अच्छा हो। उत्तर भारत में इन फसलों को मटियार दोमट मृदा से लेकर रेतीली दोमट मृदा में उगाया जाता है। इन फसलों के लिए बलुई-दोमट अथवा दोमट मृदा, जिसका pH मान 6.5-7.5 के बीच हो और भूमि जल की गहराई पर हो, सर्वोत्तम रहती है।
- दीमक नियंत्रण: यदि मृदा में दीमक की समस्या हो, तो इसके प्रकोप से बचने के लिए 20-25 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर कार्बेरिल (59 प्रतिशत) को मिट्टी में उस समय मिलाना चाहिए, जब खेत की तैयारी अंतिम चरण में हो। इसके अलावा 10 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर की दर से एल्डीकार्ब या फोरेट का प्रयोग भी लाभदायक रहता है।
- अरहर की उन्नत प्रजातियाँ: उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के लिए: पूसा अरहर 151, सीजी अरहर 2 आदि प्रमुख हैं।
- मूंग की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा 1371, पूसा रत्ना, पूसा 672, सम्राट (पीडीएम 139), पी.डी.एम. 34 आदि।
- उड़द की उन्नत प्रजातियाँ: के.यू.जी.-479, नरेन्द्र उड़द-1, एनडीयू 99-2, आजाद उड़द 1, आजाद उड़द 2, आजाद उड़द 3, शेखर उड़द 1, शेखर उड़द 2, शेखर उड़द 3 आदि।
- बीजोपचार एवं राइजोबियम जीवाणु द्वारा बीज शोधन:
- मृदा एवं बीजजनित कई कवक एवं जीवाणुजनित रोग होते हैं, जो अंकुरण के समय तथा बाद में बीजों को काफी क्षति पहुंचाते हैं।
- बीजों के अच्छे अंकुरण तथा स्वस्थ पौधों की पर्याप्त संख्या हेतु बीजों को कवकनाशी से उपचार करने की सलाह दी जाती है।
- कवकनाशी उपचार: इसके लिए प्रति किलोग्राम बीज को 2-2.5 ग्राम थीरम तथा 1 ग्राम कार्बण्डाजिम से उपचार करना चाहिए।
- राइजोबियम कल्चर से बीज शोधन: कवकनाशी उपचार के बाद राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करना चाहिए। उपचार हेतु 500 मि.ली. स्वच्छ जल में 100 ग्राम गुड़ एवं 2 ग्राम गोंद को पानी में मिलाकर गर्म कर लेना चाहिए।इसके बाद इसे ठंडा करके एक पैकेट राइजोबियम कल्चर/टीका (10 कि.ग्रा. बीज के लिए) मिलाकर अच्छी तरह बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए एवं उपचारित बीजों को छाया में सुखाना चाहिए।
- सल्फर का प्रयोग: बुआई के समय बीज डालने से पहले सल्फर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए।
- पीएसबी (PSB) द्वारा शोधन: इसी प्रकार फॉस्फेट घुलनशील बैक्टीरिया (PSB) से बीज का शोधन करना भी लाभदायक होता है।
- खरपतवार प्रबंधन: बुआई के प्रारंभिक 4-5 सप्ताह तक खरपतवार की समस्या अधिक रहती है। पहली सिंचाई के बाद निराई कर देनी चाहिए।
- रासायनिक विधि: चौड़ी पत्ती तथा घास वाले खरपतवार को रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिये निम्नलिखित शाकनाशियों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए:
- पेण्डीमेथिलीन (30 ई.सी.) 3.30 लीटर या एलाक्लोर की 4 लीटर या फ्लूक्लोरोलिन (45 ई.सी.) 2.20 लीटर या मेटोलाक्लोर (50 ई.सी.) 2.0 लीटर
- इन्हें 600-800 लीटर पानी में मिलाकर बुआई के तुरंत बाद या अंकुरण से पहले छिड़काव कर देना चाहिए।
- अरहर की फसल में विशिष्ट: अरहर की फसल में बुआई के 25 दिनों बाद निराई-गुड़ाई करके खरपतवार नियंत्रण तथा सघन पौधों को निकाल देना चाहिए (विरलन)।
- रासायनिक विधि: चौड़ी पत्ती तथा घास वाले खरपतवार को रासायनिक विधि से नष्ट करने के लिये निम्नलिखित शाकनाशियों में से किसी एक का प्रयोग करना चाहिए:
कपास (Cotton)
- कपास एक महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो व्यावसायिक क्षेत्र में श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। इसकी खेती रेतीली लवणीय तथा सेम वाली मृदा को छोड़कर सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है।
- बुआई:
- समय: उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में कपास की बुआई मानसून के आने पर ही की जाती है। हालाँकि यदि सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, तो मई में भी इसकी बुआई की जा सकती है। बुआई के लिए सीड-कम-फर्टी ड्रिल अथवा प्लांटर का प्रयोग कर सकते हैं।
- बीज दर (प्रति हेक्टेयर): अमेरिकन कपास: 15-20 कि.ग्रा., संकर कपास: 4-5 कि.ग्रा., देसी कपास: 10-12 कि.ग्रा.।
- बुआई की दूरी:
- देसी अथवा अमेरिकन कपास के लिए: 60 सें.मी.×30 सें.मी. (पंक्ति से पंक्ति × पौधे से पौधे)
- संकर किस्मों के लिए: 90 सें.मी.×40 सें.मी. (पंक्ति से पंक्ति × पौधे से पौधे)
- बीजोपचार:
- बीजों को प्रति किलोग्राम 2.5 ग्राम कार्बण्डाजिम या कैप्टॉन दवा से उपचारित कर फसल को राइजोक्टोनिया जड़ गलन, फ्यूजेरियम उकठा और अन्य मृदाजनित फफूंद से होने वाली व्याधियों से बचाया जा सकता है।
- इमिडाक्लोरोप्रिड 7.0 ग्राम अथवा कार्बोसल्फॉन 20 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज उपचार से 40-60 दिनों तक रस चूसक कीटों से सुरक्षा मिलती है।
- दीमक से बचाव के लिए 10 मि.ली. पानी में 10 मि.ली. क्लोरोपाइरीफॉस मिलाकर बीज पर छिड़क दें तथा 30-40 मिनट छाया में सुखाकर बुआई कर दें।
- किस्मों का चयन:
- संकर प्रजातियां: लक्ष्मी, एच.एस. 45, एच.एस.6, एल.एच. 144, एच.एल. 1556, एफ. 1861
- देसी प्रजातियां: एच. 777, एच.डी. 1, एच. 974 एवं एल.डी. 327 आदि प्रमुख हैं।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए।
- उर्वरक की मात्रा (प्रति हेक्टेयर):
- कपास की अमेरिकन एवं देसी किस्मों के लिये: 60-80 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 30 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 20-30 कि.ग्रा. पोटाश
- संकर किस्मों के लिये: 150 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 60 कि.ग्रा. पोटाश
- जिंक: 25 कि.ग्रा. जिंक प्रति हेक्टेयर का प्रयोग लाभदायक है।
- प्रयोग विधि और समय:
- नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं बाकी उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय डालनी चाहिए।
- नाइट्रोजन की बाकी मात्रा फूल आने के समय सिंचाई के बाद में देनी चाहिए।
चारा वाली फसलें (Fodder Crops)
- सभी चारा फसलों की बोआई मानसून के आगमन पर या तुरंत बाद करें।
- अच्छी किस्मों का चयन कर अधिक चारा उत्पादन पाएं।
- पौधों की निराई-गुड़ाई, सिंचाई व उर्वरक प्रबंधन समय पर करें।
चारा वाली फसलों की जानकारी तालिका
| फसल का नाम | प्रमुख किस्में | बोआई का समय | औसत उत्पादन क्षमता | विशेष जानकारी |
|---|---|---|---|---|
| ज्वार (चरी) | HC-136, HC-171, HC-260, हरियाणा चरी-308 | जून के अंत से जुलाई | 200 क्विंटल हरा चारा / 6 क्विंटल बीज | बहु-कटाई वाली किस्में उपलब्ध; वर्षा आधारित खेती हेतु उपयुक्त |
| बाजरा (चारा) | पूसा कम्पोजिट-443, राज बाजरा चारी-2, WCC-75, ICTP-8203 | जुलाई का दूसरा पखवाड़ा | 150–180 क्विंटल हरा चारा/हेक्टेयर | कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए उपयुक्त |
| मक्का (चारा) | African Tall, J-1006, Vijay Composite | मानसून से पूर्व या जुलाई | 350–400 क्विंटल हरा चारा/हेक्टेयर | शीघ्र वृद्धि करने वाली फसल; अच्छी जल निकासी जरूरी |
| नेपियर-बाजरा घास | नेपियर बाजरा संकर-21, CO-3, CO-4 | मॉनसून प्रारंभ | 400–500 क्विंटल हरा चारा/हेक्टेयर | बहु-वर्षीय घास, 6–7 कटाई साल में; सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त |
सब्जियों की खेती (Vegetable Farming):
फूलगोभी (Cauliflower)
- अगेती फूलगोभी की उन्नत प्रजातियाँ जिनकी रोपाई इस समय की जा सकती है, वे हैं: पूसा शरद, काशी क्वारी, अर्ली क्वारी, पूसा कार्तिकी, पूसा अर्ली सिंथेटिक।
- रोपाई की दूरी: रोपाई 45 सें.मी.×30 सें.मी. की दूरी पर करें।
- पोषक तत्व: प्रति हेक्टेयर 40 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस एवं 40 कि.ग्रा. पोटाश का प्रयोग करें।
- जल निकास: रोपित खेतों में जल निकास की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि जलभराव फूलगोभी के लिए हानिकारक हो सकता है।
हरी मिर्च (Green Chilly)
- अगेती हरी मिर्च की उन्नत प्रजातियाँ जिनकी रोपाई इस समय की जा सकती है, वे हैं: पूसा सदाबहार, काशी अनमोल, काशी गौर, पूसा ज्वाला, पंत सी-1, पंजाब लाल एवं संकर किस्में: काशी सुर्ख, काशी अगेती, काशी तेज, अर्का मेघना, अर्का हरिता।
- रोपाई की दूरी: रोपाई 45 सें.मी.×30 सें.मी. की दूरी पर करें।
- पोषक तत्व: हरी मिर्च में प्रति हेक्टेयर 40 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 40 कि.ग्रा. पोटाश की दर से प्रयोग करें।
भिंडी (Ladyfinger)
- भिंडी (Okra) एक लोकप्रिय और महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, जिसे खरीफ मौसम में उगाया जाता है।
- उन्नत किस्में: भिंडी की कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं: पूसा ए-5, परभणी क्रान्ति, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी सातधारी, काशी क्रान्ति।
- संकर किस्में (Hybrid Varieties): काशी भैरव, सारिका, सिंजेंटा-152, महिको-8888, यू.एस.-7109, एस.-5, जे.के. हरिता आदि प्रमुख हैं।
- बुआई:
- बीज दर: बुआई हेतु बीज दर 8-10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।
- बुआई की दूरी: बुआई की दूरी 60 सें.मी.×30 सें.मी. (पंक्ति से पंक्ति × पौधे से पौधे)।
- बुआई का समय: जून-जुलाई (खरीफ) का समय भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त माना जाता है।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- रासायनिक उर्वरक: प्रति हेक्टेयर 100 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 50 कि.ग्रा. फॉस्फोरस तथा 50 कि.ग्रा. पोटाश का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है।
- गोबर की खाद: यदि गोबर की खाद उपलब्ध है, तो 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। यह मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार करता है।
बैंगन (Brinjal)
- बैंगन (Brinjal/Eggplant) भारत की एक महत्वपूर्ण सब्जी फसल है, जिसे गर्म और वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। यह पाले को सहन नहीं कर सकता।
- जलवायु: यह एक गर्म और वर्षा ऋतु की फसल है, जो पाले को सहन नहीं कर सकती।
- मृदा: इसकी खेती के लिए 6 से 7 pH मान वाली बलुई दोमट, अच्छी जल निकासी वाली मृदा उपयुक्त है।
- अगेती बैंगन की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा बिंदु, पूसा कौशल, पूसा श्यामला, पूसा अंकुर।
- गोल बैंगन की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा उत्तम, काशी संदेश, पंत ऋतुराज, रामनगर जॉयन्ट आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर: अच्छी जमाव क्षमता वाला 400 ग्राम तथा 250-300 ग्राम संकर किस्मों का बीज प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होता है।
- नर्सरी का समय: बैंगन की नर्सरी जुलाई में लगाने से अक्टूबर में सब्जी मिलने लगेगी।
- रोपाई की दूरी: रोपाई 75 सें.मी.×60 सें.मी. की दूरी पर की जाती है।
- खेत की तैयारी के समय: 25 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस, 60 कि.ग्रा. पोटाश, 150 कि.ग्रा. नाइट्रोजन की आधी मात्रा, इन सभी को मिट्टी में मिला दें।
- टॉप ड्रेसिंग: बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा को फूल आने के समय प्रयोग करें।
- रासायनिक नियंत्रण: रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए पेण्डीमेथिलीन नामक खरपतवारनाशी की 3 लीटर मात्रा का प्रति हेक्टेयर की दर से पौध रोपाई से पहले प्रयोग करें।
- निराई-गुड़ाई: आवश्यकतानुसार निराई-गुड़ाई करते रहें।
कद्दूवर्गीय सब्जियां (Cucurbitaceous vegetables)
- जून के अंत से जुलाई का समय कद्दूवर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए सर्वोत्तम होता है। यह समय मानसून की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जो इन फसलों के विकास के लिए आदर्श परिस्थितियाँ प्रदान करता है।
- बुआई की विधि (नाली विधि):
- नालियां बनाना: खेत में लगभग 45 सें.मी. चौड़ी तथा 30-40 सें.मी. गहरी नालियां बना लें। ये नालियां पौधों को सहारा देने और जल प्रबंधन में मदद करती हैं।
- पानी भरना: बुआई से पहले नालियों में पानी भर दें। यह मिट्टी को नम करेगा और बीजों के अंकुरण के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा।
- नमी का आकलन: जब नाली में नमी की मात्रा बीज बुआई के लिए उपयुक्त हो जाए, तब ही बुआई करें। मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, लेकिन अत्यधिक गीलापन नहीं।
- मिट्टी भुरभुरी करना: बुआई के स्थान पर मिट्टी को भुरभुरी करके फिर बीज बोएं। इससे बीजों को अंकुरित होने और जड़ों को विकसित होने में आसानी होती है।
लौकी (Bottle Gourd)
- लौकी एक लोकप्रिय कद्दूवर्गीय सब्जी है जिसकी खेती भारत में व्यापक रूप से की जाती है।
- लौकी की कई उन्नत प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं: पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड-3, काशी गंगा, अर्का बहार आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर: लौकी का बीज दर 4-5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
- बुआई की दूरी: लौकी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 3 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 0.5 मीटर पर बुआई करें।
कद्दू (Pumpkin)
- कद्दू की कई उन्नत प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं: पूसा विश्वास, पूसा विकास, पूसा हाइब्रिड-1, अर्का चन्दन, काशी हरित आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर: कद्दू का बीज दर 3-4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
तोरई (Ridge Gourd & Smooth Gourd)
- तोरई की उन्नत प्रजातियाँ:
- चिकनी तोरई (Smooth Gourd) की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा चिकनी, पूसा स्नेहा, काशी दिव्या, पूसा सुप्रिया।
- धारीदार तोरई (Ridge Gourd) की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा नूतन, अर्का सुजात, सतपुतिया, अर्का सुमीत, पूसा नसदार।
- बीज दर: तोरई की बुआई के लिए 5.0-5.5 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।
- बुआई की दूरी: इनकी बुआई 2.5 मीटर (पंक्ति से पंक्ति) × 45-50 सें.मी. (पौधे से पौधे) की दूरी पर करें।
करेला (Bitter Gourd)
- यह एक औषधीय गुणों से भरपूर और लोकप्रिय सब्जी फसल है, जिसे गर्म और आर्द्र जलवायु में उगाया जाता है।
- करेला की उन्नत किस्में का चुने जिन्हें जुलाई के पहले सप्ताह तक लगाया जा सकता है।
- इसके 3 किलोग्राम बीज को 12-20 घंटे तक भिगोयें। यह अंकुरण को बढ़ावा देने में मदद करता है। 1.7 फीट चौड़ी नाली के दोनों तरफ बुआई करें। नालियों की आपसी दूरी 6 फीट रखें।
- 10 टन देसी खाद, आधा बोरा यूरिया, 1.5 बोरा सिंगल सुपर फॉस्फेट, आधा बोरा म्यूरेट ऑफ पोटाश इन सभी को आखिरी जुताई के समय मृदा में मिला दें।
- बीजाई के समय कीटों की रोकथाम के लिए फ्यूराडॉन मिट्टी में मिला दें।
- करेला की 60-70 दिनों में 600-700 किलोग्राम पैदावार मिल जाती है।
टिंडा (Indian Round Gourd)
- पूसा रौनक, पंजाब टिंडा, अर्का टिंडा आदि टिंडा प्रमुख की उन्नत प्रजातियाँ हैं।
- बीज दर: टिंडे के लिए बीज दर 6-7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।
खीरा (Cucumber)
- खीरे की कई उन्नत प्रजातियाँ उपलब्ध हैं, जिनमें शामिल हैं: जापानी लांग ग्रीन (Japanese Long Green), स्ट्रेटे (Straight Eight), पूसा उदय, पोइनसेट (Poinsett) आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर: खीरे की बुआई हेतु बीज दर 2.0-2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होती है।
- बुआई की दूरी: पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30-45 सें.मी. रखें।
पेठा (Ash Gourd/Winter Melon)
- यह एक और महत्वपूर्ण कद्दूवर्गीय सब्जी है, जो अपनी पौष्टिक और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है।
- पेठा की उन्नत प्रजातियाँ: पूसा श्रेयाली, पूसा उर्मी, पूसा उज्जवल, काशी धवल, काशी उज्जवल,काशी सुरभि आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर: पेठा का बीज दर 5-6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
कद्दूवर्गीय सब्जियों के लिए सामान्य प्रबंधन :
- बुआई के लगभग 25-30 दिनों बाद पौधों के बढ़वार के समय प्रति हेक्टेयर 15-20 कि.ग्रा. नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करें।
- जून में बोयी गई कद्दूवर्गीय सब्जियों में मचान बनाकर सहारा दें। यह बेलों को जमीन पर फैलने से रोकता है, जिससे फलों की गुणवत्ता बेहतर होती है और रोग का प्रकोप कम होता है।
- उचित जल निकास की व्यवस्था करें। कद्दूवर्गीय सब्जियां जलभराव के प्रति संवेदनशील होती हैं, इसलिए अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है।
कुंदरू (Ivy Gourd)
- यह एक बारहमासी बेल वाली सब्जी है जिसकी रोपाई के लिए यह समय (जुलाई) उपयुक्त है। इसकी खेती में लिंग अनुपात का ध्यान रखना और उचित पोषण प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
- कुंदरू की रोपाई के लिए जुलाई का प्रथम सप्ताह उपयुक्त है।
- कुंदरू में नर एवं मादा पौधे अलग-अलग होते हैं। अच्छी उपज लेने के लिए 10 मादा पौधों पर एक नर पौधा अवश्य लगाएँ। यह परागण और फल उत्पादन के लिए आवश्यक है।
- गड्ढे की तैयारी और पोषक तत्व प्रबंधन:
- ग्रीष्म ऋतु में 3 मीटर की दूरी पर 30 सें.मी.×30 सें.मी.×30 सें.मी. आकार के गड्ढे खोदें।
- इन खोदे गए गड्ढों में 3 कि.ग्रा. सड़ी गोबर की खाद या नाडेप खाद, 50 ग्राम यूरिया, 200 ग्राम सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम पोटाश को अच्छी तरह मिट्टी एवं बालू में मिलाकर भर दें।इस मिश्रण को 10 सें.मी. की ऊंचाई तक गड्ढों में भर दें।
- रोपाई का समय: वर्षा प्रारंभ होते ही (जुलाई के प्रथम सप्ताह तक) कलिकायुक्त विकसित कलमों (cuttings with buds) को इन तैयार गड्ढों में रोप दें
खरीफ प्याज (Kharif Onion)
- खरीफ प्याज की खेती के लिए जुलाई का महीना नर्सरी तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- खरीफ की प्याज के लिए पौधशाला में बीज की बुआई 10 जुलाई तक कर दें।
- एक हेक्टेयर की रोपाई के लिए 12-15 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। यह नर्सरी में स्वस्थ पौध तैयार करने के लिए आवश्यक मात्रा है।
अदरक और हल्दी (Ginger & Turmeric
- अदरक की फसल में, बुआई के 40 दिनों बाद प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए। यह नाइट्रोजन उर्वरक मिट्टी चढ़ाते समय देना चाहिए, जिससे पौधों को उचित पोषण मिल सके और उनका विकास बेहतर हो।
- हल्दी की फसल में, 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक का प्रयोग बुआई के 35-40 दिनों बाद करना चाहिए। इस उर्वरक को पंक्तियों के बीच में प्रयोग करें ताकि पौधों को सीधा लाभ मिल सके।
जिमीकंद / सूरन (Elephant Foot Yam) और चौलाई (Amaranth)
- जिमीकंद / सूरन की फसल में, 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक का प्रयोग बुआई के 65-70 दिनों बाद करना चाहिए। इस नाइट्रोजन को टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। यह वृद्धि के महत्वपूर्ण चरण में पौधों को आवश्यक पोषण प्रदान करता है।
- बरसात वाली चौलाई की बुआई पूरे महीने (जुलाई) की जा सकती है। यह खरीफ मौसम में खेती के लिए उपयुक्त है। इसके लिए 1.5-2.0 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
फलों की खेती (Fruit Farming):
- आम की बागवानी:
- आम की जो प्रजातियाँ तैयार हो रही हैं, उन्हें समय पर बाजार भेजने की व्यवस्था करें।
- जुलाई के आखिरी सप्ताह में आम के नए पौधों को लगाएं। यह समय मानसून के कारण मिट्टी में पर्याप्त नमी होने के कारण रोपण के लिए अनुकूल होता है।
- फल तुड़ाई के बाद वृक्षों की कटाई-छंटाई (pruning) करें। यह नई वृद्धि को बढ़ावा देता है और वृक्ष को स्वस्थ रखता है।
- सूखी एवं रोगी टहनियों को काटकर जला दें। यह रोगों और कीटों के प्रसार को रोकने में मदद करता है।
- आम में शाखा कीट (Branch Borer/Twig Borer) की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस (36 ई.सी.) की 125 मि.ली. अथवा डाई-मैथोएट (30 ई.सी.) 150 मि.ली. मात्रा को 100 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर वृक्षों पर छिड़काव करें।
- रेडरस्ट (Red Rust) तथा शूट मोल्ड (Sooty Mould) रोग की रोकथाम (आम एवं लीची में): इन रोगों की रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 0.3 प्रतिशत (100 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोलकर) या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 प्रतिशत डब्ल्यू.पी. 0.3 प्रतिशत (3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर) पेड़ों पर छिड़काव करें। रेडरस्ट एक शैवाल जनित रोग है जो पत्तियों पर लाल-भूरे धब्बे पैदा करता है, जबकि शूट मोल्ड एक फंगल रोग है जो चिपचिपे स्राव पर पनपता है, जिससे पत्तियों पर काली परत बन जाती है और प्रकाश संश्लेषण बाधित होता है।
- अमरूद:
- अमरूद के नए बाग लगाने का यह उपयुक्त समय है।
- अमरूद की कुछ उन्नत और लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं: इलाहाबाद सफेदा, सरदार, अर्का मृदुला, अर्का अमूल्या, अर्का किरण, संकर अर्का अमूल्य आदि प्रमुख हैं।
- आंवला:
- आंवला के नए बाग इस माह में लगाएँ।
- प्रजातियाँ: नरेन्द्र आंवला-4, नरेन्द्र आंवला-6, नरेन्द्र आंवला-7, नरेन्द्र आंवला-10, फ्रांसिस, कृष्णा, चकैया, कंचन (एनए-4) आदि प्रमुख हैं।
- आंवले के बागों में एफिड की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.04 प्रतिशत का घोल बनाकर पौधों पर छिड़काव करें।
- केला:
- इसके नए सकर्स खेतों में रोपें।
- बसराई ड्वार्फ, हरी छाल, रोबस्टा, कोठिया, मालभोग आदि प्रमुख हैं।
- बागवानी प्रबंधन:
- केले की खेती में अवांछित पत्तियों को निकाल देना चाहिए।
- पेड़ों पर मिट्टी चढ़ाकर जल निकास का प्रबंधन करना चाहिए।
- फल आने वाले पौधों में सहारा देने के लिए थूनियां लगानी चाहिए।
- नए बाग लगाने के लिए अच्छी एवं स्वस्थ पत्तियां, जो तलवार के आकार की हों, उत्तम किस्मों से लेकर लगानी चाहिए।
- बेर:
- बेर की प्रजाति जे.जी.-2, विलायती, उमरान, कैथली, सनोर-2 आदि का प्रयोग कर नए बाग इस माह में तैयार करें।
- बेर में मिलीबग कीट की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 36 ई.सी. 1.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- लीची:
- लीची में गूटी बांधने का कार्य करें।
- रोपाई का कार्य माह के अंत तक करें।
- प्रमुख प्रजातियाँ: बेदाना, मुजफ्फरपुर, कलकतिया, देहरादून, रोजसेन्टेड शाही, त्रिकोलिया, अझौली, ग्रीन, देसी, डी-रोज, अर्ली बेदाना, स्वर्ण रूपा, चाइना, पूर्वी, कसबा आदि हैं।
- अंगूर:
- अंगूर के बागों में मध्यम समय में पकने वाली किस्मों के फल तोड़कर बाजार भेजें।
- बाग में पानी के निकास का प्रबंध करना चाहिए।
- फल सड़न रोग की रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस 0.04 प्रतिशत (40 मि.ली. प्रति 100 लीटर पानी) तथा ब्लाइटॉक्स 0.3 प्रतिशत (300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी) का छिड़काव करें।
- पपीता:
- प्रजातियाँ: पूसा नन्हा, पूसा डिलीशियस, वाशिंगटन, हनीड्यू, रेड लेडी, पूसा मैजेस्टी, पूसा ड्वार्फ, पूसा जॉयन्ट, अर्का सूर्या आदि प्रमुख हैं।
- नीबू:
- नीबूवर्गीय के पौधों को सिल्ला, लीफ माईनर एवं सफेद मक्खी से बचाव के लिए 770 मि.ली. ऑक्सीडमेटोन-मिथाइल 27 ईसी 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
- तने एवं फल के गलने का बचाव बरसात की पहली बौछार के तुरंत बाद 0.3 प्रतिशत कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें।
- लोकाट:
- बागों में पेड़ी की कटाई-छंटाई का कार्य समाप्त करना चाहिए।
- बाग में जल निकास के लिए नालियां बना लेनी चाहिए।
- कटाई-छंटाई के बाद ब्लॉइटॉक्स-50 का छिड़काव करके कटे भागों में बोडों मिश्रण का लेप लगा देना चाहिए।
- नए बाग लगाने के लिए 2-3 प्रजातियों के पौधे एक साथ लगाने चाहिए।
- कटहल:
- कटहल के फलों को तोड़कर बाजार भेजने की व्यवस्था करें।
- जल निकास का उचित प्रबंधन करना चाहिए।
- बाग लगाने के लिए पौधों की रोपाई का कार्य शुरू कर देना चाहिए।
फूल और सुगंधित पौधे (Flowers and Fragrant Plants):
- जुलाई का महीना, जो मानसून का चरम समय होता है, बागवानी प्रेमियों के लिए फूलों और सगंधीय पौधों के प्रबंधन के लिए विशेष महत्व रखता है।
- पौधे लगाने और दोबारा गमले भरने (री-पॉटिंग) के लिए सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान वायुमंडल में उच्च आर्द्रता और पर्याप्त वर्षा नए पौधों की स्थापना और पुराने पौधों के जड़ विकास के लिए अनुकूल होती है।
- वर्षा ऋतु में उगाए जाने वाले फूल : बालसम (Balsam), गेंदा (Marigold), कॉसमॉस (Cosmos), सूरजमुखी (Sunflower), जीनिया (Zinnia), क्लियोम (Cleome), सेल्विया (Salvia)
- जरबेरा (Gerbera): पुराने पौधों को विभाजित (division) करके लगाएं। यह पौधों को पुनर्जीवित करने और नए पौधे तैयार करने का एक प्रभावी तरीका है।
- नरगिस (Narcissus): नरगिस के बल्ब का भंडारण करें। मानसून से पहले या बाद में जब पौधे निष्क्रिय हो जाते हैं, तो बल्बों को निकालकर उचित भंडारण करना चाहिए ताकि उन्हें अगले मौसम में दोबारा लगाया जा सके।
- गुलदाउदी (Chrysanthemum): गुलदाउदी में शीर्ष नोचन (Pinching/Topping) का कार्य करें। इसमें पौधे के ऊपरी सिरे को हटा दिया जाता है ताकि पार्श्व शाखाओं का विकास हो और अधिक फूल आएं।
- रजनीगंधा और ग्लैडियोलस में आवश्यकतानुसार सिंचाई, निराई-गुड़ाई करें।
- पोषक तत्वों के मिश्रण का 15 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। यह पौधों की स्वस्थ वृद्धि और भरपूर फूल उत्पादन सुनिश्चित करता है।
- जल निकास की उचित व्यवस्था करें। ये पौधे जलभराव के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे बल्ब सड़ सकते हैं।
- रजनीगंधा के स्पाइक (पुष्प डंडियों) को समय-समय पर तोड़ लें। यह नए स्पाइक के विकास को प्रोत्साहित करता है और कट फ्लावर उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है।
पशुपालन/दुग्ध विकास (Animal Husbandry/Dairy Development):
- पशुओं को गलाघोंटू (Haemorrhagic Septicaemia – HS) तथा बी.क्यू. (Black Quarter – BQ) का टीका अवश्य लगवाएँ। ये बीमारियाँ बरसात के मौसम में अधिक फैलती हैं और पशुओं के लिए जानलेवा हो सकती हैं।
- पशुओं को पेट के कीड़े मारने की दवा पिलाएँ (डीवर्मिंग)। बरसात में परजीवियों का प्रकोप बढ़ जाता है, जिससे पशुओं के स्वास्थ्य और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- पशुओं को बरसात से बचाव हेतु पूरा प्रबंध करें। उन्हें बारिश और ठंडी हवा से बचाने के लिए उचित आश्रय प्रदान करें।
- पशुशाला के फर्श तथा बिछावन को सूखा रखें। नमी और सीलन बीमारियों और संक्रमण का कारण बन सकती है। नियमित रूप से सफाई और सूखे बिछावन का प्रबंध करें।
मुर्गी पालन (Poultry Farming):
- मुर्गीपालन को नमी तथा सीलन से बचाएँ। अत्यधिक नमी और सीलन मुर्गियों में श्वसन संबंधी समस्याओं और अन्य बीमारियों को जन्म दे सकती है। सुनिश्चित करें कि मुर्गीखाना सूखा रहे और कहीं भी पानी का ठहराव न हो।
- मुर्गीखाने में उचित प्रकाश की व्यवस्था करें। पर्याप्त प्रकाश मुर्गियों के स्वास्थ्य, गतिविधि और अंडे उत्पादन के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक प्रकाश के अभाव में कृत्रिम प्रकाश का उपयोग करें।
- मुर्गीखाने एवं प्रयोग किए जाने वाले बर्तनों की धूल व गंदगी की प्रतिदिन सफाई करें। नियमित सफाई से बीमारियों के कीटाणुओं को पनपने से रोका जा सकता है और स्वच्छता बनी रहती है।
- अंडे व मीट के लिए उपयुक्त प्रजातियों का चयन करें। अपनी आवश्यकता (अंडे या मांस उत्पादन) के अनुसार उन मुर्गियों की प्रजातियों का चुनाव करें जो उस उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त हों और आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हों।