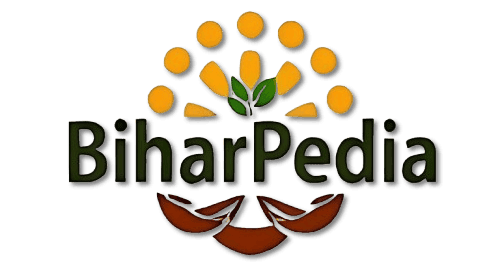अमरूद की उन्नत खेती एवं प्रबंधन (Advanced cultivation and management of Guava):
अमरूद को आमतौर पर “गरीबों के सेब” के रूप में जाना जाता है। यह अपने उच्च पोषक तत्वों के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध है। भारत में इसकी खेती हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक व्यापक रूप से की जाती है।अमरूद का उत्पादन पूरे वर्ष किया जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में उत्पादित होने वाले फल उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। अन्य प्रमुख फलों की तरह, अमरूद भी अपने मीठे स्वाद और औषधीय गुणों से भरपूर होता है, जिससे यह फलों की मुख्य श्रेणी में आता है। अमरूद का फल मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें प्रमुख रूप से विटामिन A और B, पेक्टिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, रेशा (फाइबर) और खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

अमरूद की खेती
मृदा एवं जलवायु:
अमरूद की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे रेतीली, दोमट और चिकनी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। उत्तर भारत में उच्च गुणवत्ता वाले अमरूद मुख्यतः हल्की रेतीली मिट्टी, विशेष रूप से नदी घाटियों की मिट्टी में उगाए जाते हैं। खेती के लिए 8.5 तक pH मान वाली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, जबकि लवणीय और क्षारीय मिट्टियाँ इसके लिए अनुपयुक्त होती हैं। अमरूद उष्णकटिबंधीय (Tropical) एवं उपोष्णकटिबंधीय (Subtropical) जलवायु में आसानी से उगता है। बेहतर फल गुणवत्ता के लिए दिन में धूप और रात में ठंडा तापमान (10–12°C) लाभकारी होता है। फल तुड़ाई के समय वर्षा होने से न केवल गुणवत्ता प्रभावित होती है, बल्कि फल छेदक कीट व मक्खियों का प्रकोप भी बढ़ जाता है।
मरूद की उन्नत किस्में:
भारत में अमरूद की किस्मों को दो मुख्य समूहों—सफेद गूदे वाली और गुलाबी गूदे वाली किस्मों में वर्गीकृत किया गया है। व्यावसायिक रूप से प्रमुख किस्मों में सरदार (लखनऊ-49), इलाहाबाद सफेदा, चित्तीदार, एप्पल कलर, इलाहाबाद सुर्खा, हरिझा, ललित और श्वेता शामिल हैं। इनमें सरदार, इलाहाबाद सफेदा, ललित और श्वेता किस्में पूरे भारत में उगाने के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। हरिझा किस्म विशेष रूप से बिहार में इसकी अधिक उत्पादकता के कारण लोकप्रिय है। ये किस्में स्वाद, रंग, पोषण और उत्पादन क्षमता के आधार पर किसानों के बीच काफी पसंद की जाती हैं।
V. N. R बीही (अमरूद की विशेष किस्म):
VNR नर्सरी द्वारा विकसित यह किस्म अपने बड़े आकार और कम बीज वाले फलों के लिए जानी जाती है। एक फल का औसत वजन 300 से 1000 ग्राम तक होता है। पौध रोपण के दूसरे वर्ष से ही फल देना शुरू कर देती है, जो इसे किसानों के लिए लाभकारी बनाता है। सामान्य परिस्थितियों में फल 15 दिन तक और प्रशीतन (कोल्ड स्टोरेज) में 30 दिन तक सुरक्षित रहता है। यह किस्म लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती है।
अमरूद की पौध तैयार करना:
अमरूद की पौध को व्यावसायिक रूप से बीज द्वारा और वानस्पतिक विधि (Vegetative Propagation) दोनों तरीकों से तैयार किया जाता है। हालांकि, एक सफल फल उद्यान या फल वाटिका स्थापित करने के लिए, गूटी (एयर लेयरिंग) और कलम (कटिंग) विधि का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है।
अमरूद का पौध रोपण
अमरूद का बगीचा या उद्यान तैयार करने के लिए, सबसे पहले गर्मी के मौसम में (अप्रैल-मई), 100 x 100 x 100 सेमी आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। लगभग 15 से 20 दिनों बाद, प्रत्येक गड्ढे में 20 किलोग्राम कार्बनिक खाद डाली जाती है। सामान्यतः, अमरूद के पौधों को 6 मीटर×6 मीटर की दूरी पर रोपित किया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर लगभग 277 पौधे लगाए जा सकते हैं।
अमरूद का उच्च घनत्व एवं अति उच्च घनत्व रोपण व प्रबंधन:
- उच्च घनत्व रोपण (High-Density Planting):अमरूद के पौधों को 3×1.5 मी., 3×3 मी. या 6×3 मी. की दूरी पर लगाया जाता है।
- अति उच्च घनत्व रोपण (Ultra-High-Density Planting):पौधों को 2×1 मी. की दूरी पर लगाकर एक हेक्टेयर में लगभग 5,000 पौधे रोपे जा सकते हैं।
- कटाई व छटाई का महत्व:पौधों की निरंतर कटाई-छटाई से उनके आकार और संरचना को नियंत्रित किया जाता है। इससे शाखाओं के बीच उचित दूरी बनती है, टहनियों की उलझन नहीं होती, और पौधा स्वस्थ रहता है।संतुलित छंटाई से फलन टहनियों की संख्या नियंत्रित होती है और उपज की गुणवत्ता बढ़ती है। उचित ऊँचाई बनाए रखने से तुड़ाई आसान होती है और लागत भी घटती है।
🌳 उच्च घनत्व अमरूद उद्यान का प्रबंधन (3×1.5 मी., 3×3 मी., 6×3 मी.)
🔹 1. प्रारंभिक कटाई: पौधरोपण के 1–2 महीने बाद, पौधे को मृदा की सतह से 60–70 से.मी. ऊँचाई पर काटें।
🔹 2. नई टहनियाँ चुनना: कटाई के बाद उगने वाली सभी टहनियों में से 3–4 मजबूत टहनियाँ रखें। बाकी को हटा दें।
🔹 3. टहनियों की पहली छंटाई: 3–4 महीने बाद इन टहनियों की लंबाई का 50% भाग काटें।
🔹 4. बार-बार छंटाई: हर 3–4 महीने में टहनियों की लंबाई का 50% हिस्सा काटते रहें। यह कार्य अगले 2 वर्षों तक पौधे को उचित आकार देने के लिए जारी रखें।
🔹 5. मौसमी छंटाई: जनवरी–फरवरी (शरद ऋतु फलन हेतु) और मई–जून (वर्षा ऋतु फलन हेतु)
🔹 6. वार्षिक आकार नियंत्रण: प्रत्येक वर्ष टहनियों का लगभग 50% भाग काटें ताकि पौधे की ऊँचाई, चौड़ाई और फलन क्षेत्र संतुलित रहे। यह कार्य लगातार 4–5 वर्षों तक करें।
खाद एवं उर्वरक प्रबंधन:
उच्च घनत्व वाले बगीचे या अति उच्च घनत्व वाले अमरूद के बगीचे में खाद और उर्वरक की मात्रा पौधे की उम्र, पौधे की अवस्था और मृदा के प्रकार पर निर्भर करती है। पौधों की अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए खाद और उर्वरक की मात्रा नीचे दी गई तालिका के अनुसार होनी चाहिए:
जब कतार से कतार की दूरी एवं पौध से पौध की दूरी 3 मीटर×1.5 मीटर, 3 मीटर×3 मीटर एवं 6 मीटर×3 मीटर हो, तो उर्वरक की मात्रा प्रतिवर्ष निम्नानुसार होनी चाहिए:
| वर्ष | यूरिया (ग्राम प्रति पौधा) | एस. एस. पी. (ग्राम प्रति पौधा) | एम. ओ. पी. (ग्राम प्रति पौधा) | |
|---|---|---|---|---|
| जून | सितम्बर | सितम्बर | जून | |
| 1st | 182 | 78 | 375 | 100 |
| 2nd | 364 | 156 | 750 | 200 |
| 3rd | 546 | 234 | 1125 | 300 |
| 4th | 728 | 312 | 1500 | 400 |
| 5th या ऊपर | 910 | 390 | 1875 | 500 |
2 X 1 मी. की दूरी पर उर्वरक की मात्रा
| वर्ष | यूरिया (ग्राम प्रति पौधा) | एस. एस. पी. (ग्राम प्रति पौधा) | एम. ओ. पी. (ग्राम प्रति पौधा) | |
|---|---|---|---|---|
| जून | सितम्बर | सितम्बर | जून | |
| 1st | 90 | 40 | 185 | 50 |
| 2nd | 180 | 110 | 370 | 100 |
| 3rd | 270 | 115 | 555 | 150 |
| 4th | 360 | 150 | 740 | 200 |
| 5th या ऊपर | 450 | 190 | 900 | 250 |
अतिरिक्त पोषण: अमरूद के पौधों में बेहतर वृद्धि, गुणवत्तापूर्ण फल उत्पादन और अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उचित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों के साथ-साथ पर्ण छिड़काव और सिंचाई व्यवस्था का विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। फलों की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु यूरिया का 1-2 प्रतिशत अथवा पोटेशियम सल्फेट का 1 प्रतिशत घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा, यदि गूदे में जिंक की कमी पाई जाए तो 0.45 किलोग्राम जिंक सल्फेट और 0.32 किलोग्राम बुझा चूना को 33 लीटर पानी में अच्छी तरह घोलकर मृदा में प्रयोग किया जाना चाहिए।
सिंचाई: अमरूद के नये पौधों की रोपाई के समय सिंचाई बहुत जरूरी होती है। पौधे रोपने के बाद पहले सप्ताह में प्रत्येक दूसरे दिन और अगले सप्ताह में दो बार सिंचाई करनी चाहिए। मानसून की शुरुआत के बाद सिंचाई आवश्यकता के अनुसार की जाती है। जब पौधे दो वर्ष या उससे अधिक आयु के हो जाते हैं, तब गर्मियों के मौसम में प्रत्येक 7-10 दिन और सर्दियों के मौसम में 20-25 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए।
टपक सिंचाई प्रणाली (ड्रिप इरिगेशन): पानी की कमी वाले क्षेत्रों में अमरूद की खेती के लिए टपक (ड्रिप) सिंचाई प्रणाली अत्यंत लाभकारी सिद्ध होती है। यह विधि न केवल 40 से 50 प्रतिशत तक जल की बचत करती है, बल्कि उत्पादन में भी लगभग 40 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव बनाती है। उच्च घनत्व या अति उच्च घनत्व वाले बागानों में जब पौधों की आपसी दूरी 3×1.5 मीटर, 3×3 मीटर या 6×3 मीटर हो, तब सिंचाई कार्य को योजनाबद्ध तरीके से टपक विधि द्वारा करना चाहिए।
जब अमरूद के पौधों के बीच की दूरी 3 मीटर × 1.5 मीटर, 3 मीटर × 3 मीटर एवं 6 मीटर × 3 मीटर हो, तब सिंचाई नियमानुसार करनी चाहिए:
| वर्ष | टपक सिंचाई (लीटर प्रति दिन प्रति पौधा) |
|---|---|
| 1st | 4 से 6 |
| 2nd | 8 से 12 |
| 3rd | 15 से 20 |
| 4th | 25 से 30 |
| 5th या इससे ऊपर | 35 से 40 |
अति उच्च घनत्व वाले फल उद्यान के लिये (2 मीटर × 1 मीटर):
| वर्ष | टपक सिंचाई (लीटर प्रति दिन प्रति पौधा) |
|---|---|
| 1st | 2 से 3 |
| 2nd | 4 से 5 |
| 3rd | 6 से 8 |
| 4th | 10 से 12 |
| 5th या इससे ऊपर | 14 से 16 |
गुणवत्ता में सुधार: अमरूद के फलों को कागज के थैले या पॉलीथीन के थैले से ढकने पर उसके भीतर का सूक्ष्म वातावरण बदल जाता है, जिससे फल को कीट, रोग एवं बीमारियों से भौतिक रूप से संरक्षण प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया से अमरूद के फल की गुणवत्ता में स्पष्ट सुधार होता है।
बायोफोर्टिफिकेशन: यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें मुख्य फसलों में आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिये कृषि संबंधित क्रियाएं, चयनात्मक प्रजनन या आनुवंशिक संशोधन किए जाते हैं। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य में सुधार करना है।
उदाहरण: अमरूद के पौधों पर रणनीतिक रूप से कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव कर, फलों में कैल्शियम की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को कैल्शियम की कमी से होने वाले रोगों से बचाया जा सकता है।
बायोफोर्टिफिकेशन के प्रकार
बायोफोर्टिफिकेशन फसलों में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने की एक प्रक्रिया है, जिसे मुख्य रूप से तीन तरीकों से किया जा सकता है:
- कृषि शास्त्रीय बायोफोर्टिफिकेशन (Agronomic Biofortification):
- इस विधि में कृषि पद्धतियों का उपयोग करके पौधों में पोषक तत्वों की सांद्रता बढ़ाई जाती है।
- इसमें आमतौर पर उर्वरकों का उपयोग शामिल होता है जो सीधे मिट्टी में आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व (जैसे जिंक, आयरन) डालते हैं, जिन्हें पौधे अवशोषित कर लेते हैं और फल/अनाज में जमा कर लेते हैं।
- यह एक अपेक्षाकृत तेज़ तरीका है और इसे मौजूदा फसल किस्मों पर लागू किया जा सकता है।
- उदाहरण: अमरूद के पौधे में कैल्शियम क्लोराइड का छिड़काव करके फल में कैल्शियम बढ़ाना।
- पारंपरिक प्रजनन बायोफोर्टिफिकेशन (Conventional Breeding Biofortification):
- यह विधि पारंपरिक पौधों के प्रजनन तकनीकों का उपयोग करती है।
- इसमें उच्च पोषक तत्व सामग्री वाली फसल किस्मों की पहचान की जाती है और उन्हें ऐसी किस्मों के साथ संकरित (cross-breed) किया जाता है जिनमें अन्य वांछित गुण (जैसे उच्च उपज, रोग प्रतिरोधक क्षमता) होते हैं।
- इस प्रक्रिया में कई फसल चक्र लग सकते हैं और यह अपेक्षाकृत धीमी विधि है, लेकिन इसके परिणामस्वरूप स्थायी रूप से पोषक तत्व-समृद्ध किस्में विकसित होती हैं जिन्हें किसान हर साल उगा सकते हैं।
- उदाहरण: विटामिन A से भरपूर मक्का या आयरन से भरपूर चावल की किस्मों का विकास।
- आनुवंशिक संशोधन बायोफोर्टिफिकेशन (Genetic Modification Biofortification):
- इस विधि में आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग करके फसल के डीएनए में सीधे जीन को डाला या संशोधित किया जाता है, ताकि उसमें विशिष्ट पोषक तत्वों का उत्पादन या संचय बढ़ सके।
- यह प्रक्रिया बहुत सटीक होती है और उन गुणों को पेश कर सकती है जो पारंपरिक प्रजनन के माध्यम से संभव नहीं हैं (उदाहरण के लिए, किसी अन्य प्रजाति से जीन डालना)।
- यह अपेक्षाकृत तेज़ हो सकता है लेकिन नियामक बाधाओं और सार्वजनिक स्वीकृति से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
- उदाहरण: गोल्डन राइस, जिसे विटामिन A के अग्रदूत बीटा-कैरोटीन का उत्पादन करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किया गया है।
अमरूद में प्रमुख कीट एवं बीमारियाँ
अमरूद के पौधों को कई तरह के कीट और बीमारियाँ प्रभावित कर सकती हैं, जिससे फसल को नुकसान होता है। प्रमुख रूप से पाई जाने वाली कवक जनक (फंगल) बीमारियाँ निम्नलिखित हैं:
उकठा रोग (Wilt Disease):
बीमारी के लक्षण:
इस रोग के शुरुआती लक्षणों में ऊपरी शाखाओं की पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और उनका रंग बदलकर पीला हो जाता है, जो बाद में लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद पत्तियाँ झड़ने लगती हैं।
रोगग्रस्त पौधों में फल का विकास रुक जाता है, फल कठोर हो जाते हैं और अंततः पूरा पौधा पत्ती विहीन होकर सूख जाता है और मर जाता है।
प्रबंधन:
- उद्यान में साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें।
- एस्पर जिलस नाईजर-17 को सड़ी हुई गोबर की खाद में मिलाकर
- 5 किग्रा प्रति गड्ढा की दर से रोपण के समय प्रयोग करें।
- 10 किग्रा प्रति गड्ढा की दर से वयस्क पौधों में उपयोग करें।
- AN-17 को 1 किग्रा प्रति क्विंटल FYM (गोबर खाद) में मिलाकर
- 1 मीटर × 2 मीटर × 3 मीटर आकार का बेड तैयार करें,
- इसके बाद सिंचाई करें।
यह उपाय उकठा रोग को नियंत्रित करने और अमरूद के पौधों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होते हैं।
अमरूद का एन्थ्रेक्नोज रोग (Anthracnose Disease):
बीमारी के लक्षण:
- यह रोग पौधे को ऊपर से नीचे की ओर सुखाना शुरू करता है।
- टहनियाँ, डंठल और नई पत्तियाँ सूखने लगती हैं और मरने लगती हैं, जिससे पूरी टहनियाँ सूख सकती हैं।
- फल एवं पत्तियों पर संक्रमण विशेष रूप से वर्षा ऋतु की फसल में अधिक देखा जाता है।
- कच्चे फलों पर छोटे-छोटे धब्बे उभरते हैं जो धीरे-धीरे बड़े होते जाते हैं।
- रोगग्रस्त भाग कठोर हो जाते हैं और अधिक संक्रमण होने पर फल में दरारें विकसित हो जाती हैं।
प्रबंधन:
- बोर्डो मिश्रण (3:3:50) या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% का छिड़काव 7-10 दिन के अंतराल पर करें।
- डिफोल्टन 0.3% और डाइवेन 7-78 (0.2%) का महीने में एक बार छिड़काव करें।
- तुड़ाई के बाद फलों को 500 PPM टेट्रासाइक्लिन के घोल में 20 मिनट तक डुबोकर रखें, इससे भंडारण के दौरान संक्रमण से बचाव होता है।
यह रोग अमरूद के उत्पादन और गुणवत्ता को काफी प्रभावित करता है, अतः समय पर सुरक्षात्मक उपाय अत्यंत आवश्यक हैं।
अमरूद का नासूर / व्रण / फोड़ा केंकर (Canker Disease):
बीमारी के लक्षण:
- यह रोग मुख्यतः हरे एवं कच्चे फलों पर हमला करता है।
- फल की बाहरी त्वचा पर भूरे रंग के गोलाकार धब्बे उभरते हैं, जिनसे बाद में गोल घेरे में आँसू या तरल पदार्थ निकलता है।
- यह संक्रमण केवल फल की ऊपरी सतह तक सीमित रहता है, अंदर के गूदे तक नहीं पहुँचता।
- पत्तियों पर छोटे व भूरे रंग के कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं।
- सर्दियों में नासूर के धब्बे सामान्य रूप से दिखाई देते हैं, जबकि वर्षा ऋतु में ये धब्बे छोटे एवं लाल रंग के होते हैं।
प्रबंधन:
- 1% बोर्डो मिश्रण या चूना-गंधक मिश्रण का 3-4 बार छिड़काव करें।
- छिड़काव का 15-15 दिन के अंतराल पर नियमित रूप से पालन करें।
यह रोग अमरूद की बाजार में बिक्री योग्य गुणवत्ता को नुकसान पहुँचा सकता है, अतः समय रहते नियंत्रण जरूरी है।
फाइटोफ्थोरा फल सड़न (Phytophthora Fruit Rot):
बीमारी के लक्षण:
- यह रोग मुख्यतः उन फलों में होता है जो सतह पर पड़े होते हैं, विशेषकर निचले भाग (Stylar end) से संक्रमण शुरू होता है।
- वे फल जो पत्तियों से ढके रहते हैं या जिनका कोई भाग मिट्टी को छूता है, उनमें संक्रमण की संभावना अधिक होती है।
- अत्यधिक नमी या आद्रता वाले मौसम में यह रोग तेजी से फैलता है और 3-4 दिनों में पूरे फल को संक्रमित कर देता है।
- शुरुआत में फल की त्वचा पर सफेद रुई जैसी फफूंद दिखाई देती है।
- धीरे-धीरे यह कोमल होकर हल्के भूरे से गहरे भूरे रंग में परिवर्तित हो जाती है।
- संक्रमित फल से दुर्गंध (अप्रिय गंध) आने लगती है।
प्रबंधन:
- इस रोग की रोकथाम हेतु डायथेन Z-78 @ 0.2% (10 PPM) का छिड़काव प्रभावी माना जाता है।
- छिड़काव आद्रता बढ़ने से पहले या संक्रमण के शुरुआती संकेत मिलने पर करना चाहिए।
सावधानी: खेत की सफाई, फल को मिट्टी से दूर रखना, और जल निकासी की उचित व्यवस्था इस रोग के प्रसार को रोकने में सहायक होती है।
स्टाइलर एंड रॉट (Stylar End Rot):
बीमारी के लक्षण:
- इस रोग की शुरुआत फल के निचले भाग (स्टाइलर एंड) से होती है, जो रंगहीन हो जाता है।
- कुछ ही समय में यह भाग धीरे-धीरे बढ़ते हुए गहरे भूरे रंग में बदल जाता है और अत्यधिक कोमल हो जाता है।
- संक्रमण बढ़ने पर फल सिकुड़ने लगता है और उस पर झुर्रियाँ दिखाई देती हैं।
- अंततः पूरा फल भूरे रंग का हो जाता है, और खाने योग्य नहीं रह जाता।
प्रबंधन:
- रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड @ 0.3% का हर 15 दिन में छिड़काव करें।
- साथ ही, कार्बेन्डाजिम @ 0.1% का दो बार छिड़काव करें, दोनों के बीच 15 दिनों का अंतराल रखें।
- अंतिम छिड़काव फलों की तुड़ाई से 12-15 दिन पहले अवश्य कर लें।
सावधानियाँ:
- जल निकासी की उचित व्यवस्था,
- फल को मिट्टी से संपर्क में न आने देना,
- तथा पौधों का उचित वायुसंचार बनाए रखना इस रोग की रोकथाम में सहायक होते हैं।
अनार की तितली (Pomegranate Butterfly)
कीट परिचय एवं हानि:
अनार की तितली वर्षा (अगस्त) और सर्दियों (नवम्बर-दिसम्बर) के मौसम में अमरूद के फलों पर गंभीर हमला करती है। बैंगनी रंग की मादा तितली फल और पुष्पकोश पर सफेद चमकीले अंडे देती है।
इनसे निकला लार्वा (डिंभक) फल को छेदकर उसके गूदे और बीज को खा जाता है, जिससे फल अंदर से खोखला हो जाता है और खराब हो जाता है।
प्रबंधन:
- संक्रमित फलों को समय-समय पर इकट्ठा कर नष्ट करें।
- अमरूद के बगीचे के पास अनार की खेती को सीमित या बंद करें क्योंकि यह कीट वहीं से आता है।
- रासायनिक नियंत्रण:
- कार्बारिल @ 0.2% या
- इथेओफेन प्रॉक्स @ 0.05%
- का छिड़काव दो बार करें — एक बार फल लगने से पहले, और दूसरी बार फल पकने से पहले।
सावधानी:
- छिड़काव सुबह या शाम के समय करें।
- फलों की तुड़ाई से कम से कम 10-12 दिन पहले अंतिम छिड़काव करें।
तना छेदक (Stem Borer):
कीट के लक्षण:
तना छेदक का प्रमुख लक्षण है — पौधे के नीचे के हिस्से में भूसे जैसे रंग का गोलीनुमा मल पदार्थ दिखाई देना। साथ ही 1-1.5 मिमी व्यास के छोटे-छोटे छिद्र, जो 20 से 30 से.मी. दूरी तक पाए जाते हैं।
गंभीर संक्रमण में पत्तियाँ झड़ने लगती हैं, टहनियाँ और शाखाएँ सूखने लगती हैं और अंततः पौधा मर सकता है।
मादा कीट शाखा में छेद करके अंडे देती है, जिनसे निकला लार्वा पहले छाल खाता है, फिर मुख्य तने में प्रवेश कर वक्राकार सुरंग बनाता है।
प्रबंधन:
- भृंग/झींगुर को यांत्रिक विधि से नष्ट करें।
- दिसम्बर से फरवरी के बीच संक्रमित शाखाओं को काटकर जला देना चाहिए।
- गंभीर प्रकोप की स्थिति में डाइक्लोरोवास @ 0.1% (5 मि.ली.) का इंजेक्शन छिद्रों में लगाएं।
- सितम्बर-अक्टूबर में तनों पर बने U आकार के छिद्रों वाले भाग को पहचानकर नष्ट करें, क्योंकि वहाँ अंडे पाए जाते हैं।
सावधानी:
- कीट की पहचान जल्द से जल्द करें ताकि प्रकोप फैलने से रोका जा सके।
- रसायनों के उपयोग के समय सुरक्षा उपाय अपनाएं।
अमरूद में लगने वाले कीट की पहचान एवं प्रबंधन
फल मक्खी (Fruit Fly):
पहचान:
वर्षा ऋतु में अमरूद की खेती में फल मक्खी (Bactrocera spp.) एक गंभीर कीट समस्या बन जाती है। मादा मक्खी पके हुए फलों की बाहरी सतह पर थोड़ा अंदर तक अंडे देती है, जिससे वहां गहरे गड्ढे जैसे निशान बन जाते हैं।
अंडों से कीड़े (लार्वा) निकलकर फल के गूदे को खाते हैं, जिससे फल खपत योग्य नहीं रहता। ये कीड़े मृदा में जाकर प्यूपा बनते हैं और 12–18 दिनों में जीवनचक्र पूरा करते हैं, विशेषकर जुलाई-अगस्त में।
प्रबंधन:
- संक्रमित फलों को इकट्ठा कर नष्ट करें।
- पौधे के चारों ओर गहरी जुताई करें, ताकि प्यूपा सूर्य की रोशनी से नष्ट हो जाए।
- प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट (0.2-0.25%) का छिड़काव करें, जिससे वयस्क मक्खियाँ मर जाएं।
- इथेनॉल:मेथिल यूगेनॉल:मैलाथियान (6:4:1) के मिश्रण में लकड़ी के ब्लॉक भिगोकर 10 ट्रैप प्रति हेक्टेयर लगाएं, और उन्हें 72 घंटों तक पेड़ पर टांगें।
यह उपाय फल मक्खी की जनसंख्या को नियंत्रित करने में प्रभावी होते हैं और अमरूद की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार लाते हैं।
छाल खाने वाली इल्ली (Bark Eating Caterpillar):
बीमारी के लक्षण:
छाल खाने वाली इल्ली प्रमुख रूप से तना, डंठल एवं शाखाओं को खाती है। इसके प्रकोप से मुख्य शाखाओं एवं टहनियों में अनियमित सुरंगें तथा धब्बे बन जाते हैं। ये सुरंगें अक्सर रेशेदार धागों और मलमूत्र से ढकी होती हैं।
प्रभावित पौधों की टहनियों और शाखाओं के जोड़ पर छिद्र आमतौर पर पाए जाते हैं। गंभीर संक्रमण की स्थिति में नई टहनियाँ सूखकर मरने लगती हैं, जिससे पौधे की वृद्धि रुक जाती है।
प्रबंधन:
- उद्यान को स्वच्छ और स्वस्थ बनाए रखें।
- बोरर छिद्रों में नेचुरेलिस-एल (0.40%) का कोनीडियल सस्पेंशन प्रभावी रहता है।
- लोहे की छड़ से छिद्रों में इल्ली को यांत्रिक रूप से नष्ट करें।
- उसके बाद रुई या ऊन को डाईक्लोरोवास (0.25-0.5%) के घोल में भिगोकर छिद्रों में भरें।
- अंत में छिद्रों को गीली मिट्टी से पूरी तरह बंद कर दें।
इस प्रकार, समय पर उचित देखभाल और नियंत्रण उपाय अपनाकर इस कीट से अमरूद के पौधों की रक्षा की जा सकती है।
निष्कर्ष
अमरूद की उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन पर आधारित इस लेख से यह स्पष्ट होता है कि अमरूद भारतीय किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फलवाली फसल है, जो सही तकनीकी विधियों को अपनाकर उच्च उत्पादन और बेहतर गुणवत्ता प्रदान कर सकती है। इसकी खेती के लिए उचित भूमि चयन, संतुलित उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन, रोग एवं कीट नियंत्रण, पौधों की नियमित कटाई-छंटाई और संरचना प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है।
उन्नत किस्मों का चयन, समयबद्ध सिंचाई, तथा वैज्ञानिक पद्धतियों का पालन फसल की उत्पादकता में वृद्धि करता है। साथ ही, खेती में तकनीकी सहायता और विशेषज्ञों की सलाह को अपनाकर किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं।
संशोधित कृषि तकनीकों और प्रबंधन उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन अमरूद की सफल एवं लाभकारी खेती सुनिश्चित कर सकता है।