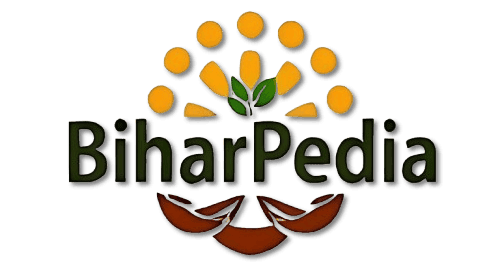जून (ज्येष्ठ-आषाढ़) माह के प्रमुख कृषि कार्य (Agricultural work in June Month):
जून में खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी शुरू होती है, जिसमें धान की नर्सरी, चारा फसलों (मक्का, ज्वार, बाजरा, लोबिया, ग्वार, लूसर्न), तिलहनी फसलों (सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, अरण्डी), और रेशेदार फसलों (कपास, जूट) की बुआाई के लिए प्रबंधन किया जाता है। मानसून आने के बाद खरीफ फसलों की पौध रोपाई जुलाई में की जाती है। अच्छी पैदावार के लिए उन्नत सस्य क्रियाओं को अपनाना आवश्यक है। मौसम के अनुसार कृषि कार्यों की योजना एवं परामर्श पर विशेष ध्यान दें। मौसम की अनिश्चितता, विशेषकर मानसून में, खरीफ फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। अतः आकस्मिक फसल योजना (Contingency Plan) के तहत बीज, खाद व अन्य संसाधनों की अग्रिम व्यवस्था रखें, ताकि किसी भी स्थिति में वैकल्पिक फसलें ली जा सकें।
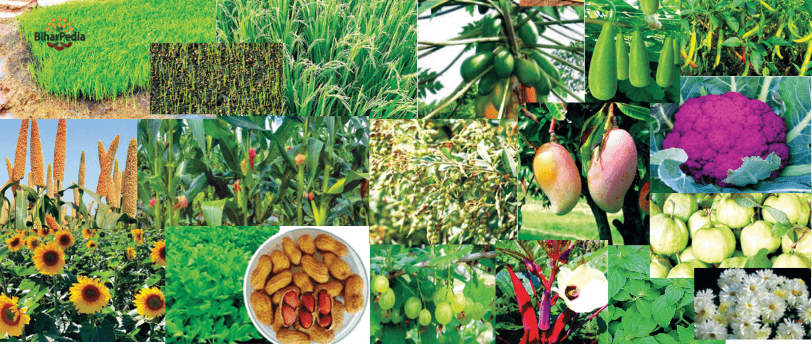
फसल उत्पादन (Crop Production):
धान की नर्सरी (Paddy Nursery)
- उपयुक्त मृदा का चयन
- धान की खेती के लिए चिकनी या मटियार मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है।
- मृदा का पीएच मान 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए।
- नर्सरी के लिए ऐसी दोमट मृदा चुनें जिसमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो और पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा हो।
- नर्सरी स्थल सिंचाई के स्रोत के पास होना चाहिए।
- नर्सरी की तैयारी
- बुआई से एक महीना पहले नर्सरी क्षेत्र की तैयारी शुरू करें।
- गर्मियों में खेत की 3-4 बार जुताई करें और उसे कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ दें। इससे मृदा जनित रोगों में कमी आती है।
- जुताई के बाद पलेवा (पानी भरकर) दें, फिर पतली जल परत बनाए रखते हुए एक दिन के लिए खेत छोड़ दें।
- क्यारियों का निर्माण
- क्यारी की चौड़ाई 1.5–2.0 मीटर और लंबाई 8–10 मीटर रखें।
- अलग-अलग किस्मों की नर्सरी बनाते समय, उनके बीच 1.5–2.0 मीटर का अंतर अवश्य रखें, ताकि प्रजातियों की मिलावट से बचा जा सके।
- क्यारियों की उचित देखभाल से पौध स्वस्थ, रोगमुक्त एवं उत्पादनक्षम बनती है।
- मृदा शोधन (Soil Treatment): मृदा शोधन के लिए ट्राइकोडर्मा/ब्यूवेरिया (2.5-3.0 कि.ग्रा.) या क्लोरोपायरीफॉस (2.5-3.0 ली./है.) का प्रयोग करें। इससे बीज और मृदाजनित रोगों से बचाव होता है व जमाव अच्छा होता है।
- बीज का चयन: धान की अच्छी पैदावार के लिए प्रमाणित एवं उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन अत्यंत आवश्यक है। ऐसे बीजों में पंक्तिबद्ध जमाव, प्रजाति की शुद्धता एवं रोगमुक्तता की गारंटी होती है।
- बीज की मात्रा (हैक्टर अनुसार):
- मोटे दानों वाली किस्में: 30–35 कि.ग्रा./हेक्टेयर
- बासमती किस्में: 20–25 कि.ग्रा./हेक्टेयर
- एक हेक्टेयर रोपाई हेतु नर्सरी क्षेत्र: 500 वर्ग मीटर पर्याप्त
- बीजोपचार विधि: बीजों को बीज जनित रोगों से बचाने हेतु निम्न उपचार करें:
- 10 लीटर पानी में मिलाएँ:
- इमिसान: 5 ग्राम (या बाविस्टीन: 10 ग्राम)
- पोसामाइसिन: 2.5 ग्राम (या विकल्प में स्टैप्टोसाइक्लीन 1 ग्राम या एग्रीमायसिन 2.5 ग्राम)
- 20–25 कि.ग्रा. बीज इस घोल में 24 घंटे भिगोकर रखें।
- भिगोने के बाद बीजों को 24–36 घंटे अंकुरित होने दें।
- अंकुरण के दौरान बीजों पर हल्का पानी छिड़कते रहें ताकि नमी बनी रहे।
- अंकुरित बीजों को नर्सरी क्यारियों में पतली पानी की सतह पर समान रूप से छिड़कें।
- 10 लीटर पानी में मिलाएँ:
- प्रारंभिक देखभाल:
- जब तक नवपौध पूरी तरह हरी न हो जाए, तब तक पक्षियों से सुरक्षा हेतु सावधानी बरतें।
- अंकुरित बीजों को शुरुआत के 2–3 दिनों तक पुआल से ढँकें।
- यह प्रक्रिया जड़ गलन, झोंका रोग और पत्तियों के झुलसा रोग से सुरक्षा देती है।
- बुआई का उपयुक्त समय:
- बुआई का समय किस्म के अनुसार थोड़ा भिन्न हो सकता है।
- सामान्यतः 15 मई से 25 जून तक का समय धान की बुआई के लिए उपयुक्त होता है।
- पोषक तत्व प्रबंधनः अच्छी फसल के लिए संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग आवश्यक है। 1000 वर्गमीटर क्षेत्र में 10 क्विंटल सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 कि.ग्रा. डाई-अमोनियम फॉस्फेट और 2.5 कि.ग्रा. जिंक सल्फेट जुताई से पहले मिट्टी में मिलाएं। 10-12 दिनों बाद यदि पौधों का रंग पीला हो, तो 10 कि.ग्रा. यूरिया/1000 वर्ग मीटर की दर से दो बार मिट्टी में मिलाएं।
- खपतवार प्रबंधनः धान नर्सरी में बुआई के 1-2 दिन बाद पायराजोसल्फ्यूरॉन (250 ग्राम/है.) को 10-15 किग्रा रेत में मिलाकर छिड़कें, फिर 1-2 सेमी हल्का पानी भरें ताकि खरपतवार नष्ट हों।
- प्रजाति अनुसार रोपाई समय:
- मध्यम एवं देर से पकने वाली किस्में: जुलाई के पहले पखवाड़े तक रोपाई पूरी करें।
- शीघ्र पकने वाली किस्में: जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक रोपाई की जा सकती है।
- सुगंधित किस्में (जैसे बासमती): जुलाई के अंत में रोपाई प्रारंभ करें।
- मृदा पोषण प्रबंधन: प्रति वर्ष, धान-गेहूं लेने वाले खेतों में 100–120 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद या हरी खाद का प्रयोग अवश्य करें, जिससे मृदा की उर्वरता बनी रहे।
- धान की पौध रोपाई और उखाड़ना:
- पौध की उपयुक्त आयु
- 20–25 दिन की आयु वाली पौध मुख्य खेत में लगाना सबसे उपयुक्त होता है।
- ज्यादा उम्र की पौध लगाने से फुटाव (tillering) कम होता है।
- पौध उखाड़ने की विधि
- रोपाई से एक दिन पहले नर्सरी में सिंचाई करें।
- पौध उखाड़ते समय कमजोर, रोगग्रस्त या अन्य किस्मों की पौध को अलग करें।
- पौध को 5–8 से.मी. व्यास के नरम बंडलों में बाँधें।
- रोपाई का तरीका
- पंक्ति से पंक्ति दूरी: 20–30 सेमी, पौधे से पौधे दूरी: 15 सेमी
- 3 से.मी. गहराई में रोपाई करें।
- प्रत्येक स्थान पर 2–3 पौधे लगाएं।
- 1 वर्ग मीटर में कम से कम 33 पौधे होने चाहिए।
- सुझाव: पौध की जड़ों को उखाड़ते समय चोट न पहुँचे, अन्यथा फसल की वृद्धि पर असर होगा।
- पौध की उपयुक्त आयु
- किस्मों का चयनः अच्छी पैदावार और गुणवत्ता के लिए प्रजाति का चयन बहुत आवश्यक है। जल स्रोत, फसलचक्र और बाज़ार की मांग को ध्यान में रखते हुए किस्में चुनें।
- खाद एवं उर्वरक की मात्राः धान की अधिक पैदावार के लिए नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और जिंक का संतुलित उपयोग करें। बौनी किस्मों के लिए 100-120 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फॉस्फोरस, 50 किग्रा पोटाश और 25 किग्रा जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर दें। बासमती की लम्बी किस्मों के लिए 60 कि.ग्रा. नाइट्रोजन पर्याप्त होती है। यूरिया को तीन हिस्सों में – रोपाई के बाद, कल्ले निकलने पर और फूल आने से पहले दें। जैविक खाद के प्रयोग पर नाइट्रोजन की मात्रा घटाएं।
धान की सीधी बुआई (Direct Seeding of Rice – DSR):
- सीधी बुआई विधि में नर्सरी की आवश्यकता नहीं होती — बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं।
- यह तकनीक श्रम और लागत दोनों की बचत करती है।
- प्रति एकड़ लगभग ₹6000 तक की लागत में कमी आती है।
- 30% तक कम पानी की आवश्यकता होती है, हालांकि शुरुआती दिनों में लगभग रोज सिंचाई करनी पड़ती है।
- रोपाई के समय 4-5 से.मी. पानी की गहराई बनाए रखना चाहिए।
- DSR दो तरीकों से किया जा सकता है:
- सूखा-DSR (Dry-DSR)
- गीला-DSR (Wet-DSR)
- यह विधि पारंपरिक धान रोपाई की तुलना में जुताई और फसल स्थापना के तरीके में भिन्न होती है।
सूखी डीएसआर विधि (Dry-DSR Method)
- इस विधि में धान की बुआई बिना नर्सरी और जलभराव के की जाती है।
- बीजों को सूखी मिट्टी में सीधे बोया जाता है।
उपयोग की जाने वाली प्रमुख तकनीकें:
- ✅ जीरो टिलेज (बिना जुताई के सीधे बीज बोना)
- ✅ पारंपरिक जुताई के बाद सूखे बीजों का प्रसारण
- ✅ डिबल्ड विधि: अच्छी तरह तैयार खेत में बीजों को हाथ या यंत्र से एक-एक कर बोना
- ✅ ड्रिलिंग विधि: पंक्तियों में मशीन से बीजों की बुआई
🔄 यह विधि पानी और श्रम की बचत करती है, लेकिन अच्छी खेत तैयारी और समय पर सिंचाई जरूरी होती है।
💧 गीला डीएसआर विधि (Wet DSR Method)
- इस विधि में अंकुरित बीजों को पोखरयुक्त (Puddled) मृदा में बोया जाता है।
प्रमुख प्रकार:
- ✅ एरोबिक गीला डीएसआर:
- अंकुरित बीजों को मृदा की सतह पर बोया जाता है।
- बीज वायवीय (Aerobic) वातावरण में अंकुरित होते हैं।
- ✅ एनारोबिक गीला डीएसआर:
- बीजों को मृदा में दबाकर बोया जाता है।
- बीज अवायवीय (Anaerobic) वातावरण में बढ़ते हैं।
बीज बोने की तकनीकें:
- 📌 बीज प्रसारण (Broadcasting)
- 📌 इम सीडर 81 (IM Seeder 81) या
- 📌 अवायवीय सीडर द्वारा फरों ओपनर (Furrow Opener) का उपयोग
🔍 यह विधि पारंपरिक रोपाई की तुलना में कम श्रम और समय लेती है, लेकिन मृदा की नमी और तैयारी पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है।
एरोबिक धान विधि की पूरी जानकारी (Aerobic Rice Farming)
- 🚿 सिंचित व वर्षा जल की कमी को देखते हुए यह विधि लाभदायक है।
- ✅ सीधी बुआई: देसी हल, सीड ड्रिल या पैडी ड्रम सीडर से सीधे खेत में बुआई की जाती है।
- 📅 बुआई का समय: जून माह उपयुक्त।
- 📌 बीज मात्रा: 25–30 कि.ग्रा./हैक्टर
- 📏 पंक्ति दूरी: 25×10 सें.मी.
- 🌱 खाद सिफारिश:
- 120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन
- 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस
- 60 कि.ग्रा. पोटाश
- 25–30 कि.ग्रा./हैक्टर जिंक सल्फेट
🌿 यह विधि कम पानी में अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के साथ अपनाई जाती है और सूखे क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी है।
ग्रीष्मकालीन मक्का, ज्वार एवं बाजरा(Summer Maize, Sorghum and Millet):
- मक्का (Maize):
- दाने वाली मक्का की कटाई तब करें जब भुट्टों की ऊपरी पत्तियाँ सूखने लगें और दाने सख्त हो जाएं (25-30% नमी)।
- कटाई के बाद भुट्टों को एक सप्ताह तक धूप में सुखाएं।
- सुखाने के बाद कॉर्नशेलर से दाने अलग करें।
- बेबीकॉर्न की तुड़ाई रेशा (सिल्क) निकलने के 2–3 दिन बाद करें।
- स्वीटकॉर्न की तुड़ाई रेशा निकलने के लगभग 20–22 दिन बाद करें, जब शर्करा की मात्रा सबसे अधिक होती है।
- ज्वार (Sorghum):
- हरे चारे के लिए पहली कटाई बुआई के 50–60 दिनों बाद करें।
- इसके बाद हर 30–35 दिन में कटाई करें (कुल 3 कटाइयाँ संभव)।
- बीज के लिए एक बार ही कटाई करें।
- फूल आने की अवस्था में कटाई करने से पौष्टिक चारा मिलता है।
- लोबिया का हरा चारा फली बनने की अवस्था (2–3 माह बाद) में काटें।
- बाजरा (Pearl Millet):
- फूल आने से पहले बाजरे की फसल को चारे के लिए काटें।
- यदि इस समय न काट सकें तो 50% फूल आने पर जरूर काटें।
- बुआई के 65–70 दिन बाद फसल कटाई के लिए तैयार हो जाती है।
खरीफ मक्का, ज्वार, बाजरा और अन्य श्रीअन्न:
- मक्का:
- मक्का की बुआई के लिए, देर से पकने वाली किस्मों को मध्य मई से मध्य जून तक पलेवा करके बोना चाहिए ताकि बारिश से पहले पौधे ठीक से स्थापित हो जाएं और 15 दिन बाद निराई हो सके। शीघ्र पकने वाली किस्मों की बुआई जून के अंतिम सप्ताह तक कर लेनी चाहिए।
- खेत की तैयारी: खरीफ के मौसम में मक्का के लिए, खेत को तैयार करने के लिए हैरो से एक गहरी जुताई और उसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 जुताई पर्याप्त होती हैं। जुताई के बाद पाटा लगाना ज़रूरी है ताकि खेत में नमी बनी रहे।
- उपयुक्त मिट्टी: मक्का की खेती के लिए दोमट से लेकर बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी गहरी, भारी गठन वाली होनी चाहिए, जिसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी हो और जल निकासी की उचित सुविधा हो। लवणीय और क्षारीय मिट्टी मक्का की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है।
- खरीफ मक्का की उन्नत संकर प्रजातियां:
- जल्दी पकने वाली (85-95 दिन): पीईएचएम 2, 3, 5, विवेक संकर मक्का 4, ये सिंचित और वर्षा आधारित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है।
- पूर्णकालिक परिपक्वता (100-110 दिन): पूसा जवाहर संकर मक्का-1, गुजरात आनंद व्हाइट मक्का हाइब्रिड-2, एमएम 9344, पूसा एचएम-9 इम्प्रूव्ड, प्रताप मक्का-9, कंचन-2, डब्ल्यूसी-236; समय पर सिंचाई और वर्षा सुनिश्चित क्षेत्रों में।
- प्रोटीनयुक्त प्रजातियां: एचक्यूपीएम -1, 4, 5, 7, विवेक क्यूपीएम- 9, शक्तिमान- 1, 3, 4। ये सिंचित क्षेत्रों व समय पर बुआई हेतु उपयुक्त होता है।
- विशेष प्रकार:
- बेबीकॉर्न: पूसा संकर 2, 3, एचएम-4, बीएल-42, जी-5414।
- पॉपकॉर्न: पर्ल पॉपकॉर्न, अम्बर पॉपकॉर्न।
- स्वीटकॉर्न: प्रिया, माधुरी।
- खरीफ मक्का की बुआई और बीज प्रबंधन:
- खरीफ मक्का में प्रति हेक्टेयर 65,000 से 78,000 पौधे प्राप्त करने के लिए 20-25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है।
- बुआई गहराई: 4-5 सेमी (सामान्य: 3.5 सेमी हल के पीछे कूड़ों में)।
- दूरी:
- बीज उत्पादन: पंक्ति से पंक्ति 60-75 सेमी, पौधे से पौधा 12-15 सेमी।
- सामान्य बुआई:
- अगेती किस्में: पंक्ति 45 सेमी, पौधा 20 सेमी।
- मध्यम/देर से पकने वाली: पंक्ति 60 सेमी, पौधा 25 सेमी।
- संकर बीज उत्पादन: नर:मादा बीज 2:4 पंक्तियों में बोएं।
- मक्का में उर्वरक प्रबंधन:
- उर्वरक मात्रा: उर्वरक का प्रयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करें। सामान्यतः 120-150 किग्रा नाइट्रोजन, 75 किग्रा फॉस्फोरस, 75 किग्रा पोटाश/है.
- प्रयोग समय:
- नाइट्रोजन: 1/4 बुआई से पहले, शेष दो बराबर हिस्सों में टॉप ड्रेसिंग (घुटना ऊंचाई और जड़ें निकलने पर)।
- फॉस्फोरस और पोटाश: पूरी मात्रा बुआई से पहले।
- जैविक खाद: 6-8 टन/है. गोबर खाद बुआई से 15-20 दिन पहले, इससे नाइट्रोजन की आवश्यकता 25% कम हो सकती है।
- जिंक: 20-25 किग्रा जिंक सल्फेट/है. अंतिम जुताई में, यदि कमी के लक्षण हों।
- मक्का में सिंचाई: मक्के की अच्छी पैदावार के लिए सिल्किंग से दाना बनने तक और प्रारंभिक वृद्धि अवस्था में नमी आवश्यक होती है। यदि बारिश न हो तो सिंचाई अवश्य करें। बारिश के बाद जल निकासी की व्यवस्था ज़रूरी है, वरना पौधे पीले पड़ सकते हैं।
- खरपतवार प्रबंधन: खरपतवार नियंत्रण के लिए दो बार निराई-गुड़ाई करें—पहली 15-20 दिन और दूसरी 35-40 दिन बाद। इससे खरपतवार कम होते हैं और जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है। रासायनिक नियंत्रण के लिए एट्राजीन (1.5–2.0 कि.ग्रा./हेक्टेयर) या एलाक्लोर (4–5 ली./हेक्टेयर) का छिड़काव 600-800 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2-3 दिन बाद, अंकुरण से पूर्व करें। अगर अंकुरण हो चुका हो, तो टोपरामीजोन (33.6% सक्रिय तत्व) या टेम्बोट्रिओन (50 ग्राम सक्रिय तत्व) प्रति एकड़, 500-600 ली. पानी में, बुआई के 20-30 दिन बाद छिड़काव करें।
- महत्वपूर्ण नोट: यदि आप मक्का के बाद आलू की खेती करना चाहते हैं, तो एट्राजीन का प्रयोग न करें।
- ज्वार की खेती:
- जलवायु: शुष्क जलवायु में सफल; 25-35°C तापमान और 40-60 से.मी. वार्षिक वर्षा उपयुक्त।
- मिट्टी: हल्की दोमट, बलुई दोमट या भारी दोमट, जिसमें अच्छा जल निकास हो।
- बुआई समय: जून के अंत से जुलाई के पहले सप्ताह तक। बारानी क्षेत्रों में वर्षा के तुरंत बाद बुआई करें।
- बीज मात्रा: संकर प्रजातियों के लिए 8-9 कि.ग्रा./हेक्टेयर और सामान्य के लिए 10-12 कि.ग्रा./हेक्टेयर।
- दूरी: 45×15 से.मी.; प्रति हेक्टेयर लगभग 1,50,000 पौधे।
- बीज उपचार: कार्बेन्डाजिम, एग्रोसन जीएन या कैप्टन से 2-5 ग्राम/किग्रा बीज के हिसाब से शोधित करें; साथ ही एजोस्पिरिलम व पीएसबी से जैविक उपचार करने से उपज 15-20% तक बढ़ती है।
- ज्वार की प्रजातियाँ: संकर प्रजातियाँ जैसे CSH 16, SPV-462। चारे वाली प्रजातियाँ जैसे Maldandi (मल्दांडी), पूसा चरी-6, पन्नी संकर ज्वार-5।
- उर्वरक प्रबंधन: सिंचित क्षेत्र के लिए 100-120 kg नाइट्रोजन, 50-60 kg फॉस्फोरस, 50-60 kg पोटाश/हेक्टेयर। असिंचित क्षेत्र के लिए 50-60 kg नाइट्रोजन, 30-40 kg फॉस्फोरस, 30-40 kg पोटाश/हेक्टेयर। सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए 0.2% जिंक व 0.15% आयरन का पर्णीय छिड़काव, बुआई के 35-40 दिन बाद करे।
- जैविक खाद: गोबर/कम्पोस्ट खाद 10 टन/हेक्टेयर, बुआई से 15-20 दिन पहले खेत में मिलाएं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता व जलधारण क्षमता बढ़ती है।
- बाजरा की खेती:
- जलवायु और मृदा: शुष्क, 28-32°C, दोमट मृदा, अच्छा जल निकास।
- खेत तैयारी: 20-22 टन गोबर खाद, 2-3 हैरो जुताई, समतल भूमि।
- बुआई: 15 जून-15 जुलाई, 4-5 किग्रा/है., 45×10-12 सेमी दूरी, 2-3 सेमी गहराई, 1.75-2 लाख पौधे/है.
- प्रजातियां: पूसा 23, 415, 605, एचएचबी 50, 67, बलवान 4903।
- पोषक तत्व: संकर: 80-90 किग्रा नाइट्रोजन, 50 किग्रा फॉस्फोरस, 50 किग्रा पोटाश/है., संकुल: 20 किग्रा नाइट्रोजन, 25 किग्रा फॉस्फोरस, 25 किग्रा पोटाश/है.। थायोयूरिया 0.1% छिड़काव (30-35 दिन, सिट्टा बनने पर)।
- श्रीअन्न फसलों की बुआई:
- फसलें: कोदो (10-12 किग्रा/है.), चीना, मडुआ, रागी, सांवा (8-10 किग्रा/है.).
- तैयारी: जून में बुआई की तैयारी शुरू करें।
ग्रीष्मकालीन मूंगफली (Summer Peanuts)
- ग्रीष्मकालीन मूंगफली:
- खुदाई का समय: जब छिलके पर नसें उभरें और भीतरी भाग कत्थई हो जाए।
- प्रक्रिया: खुदाई के बाद फलियों को सुखाएं।
- भंडारण सावधानी: गीली मूंगफली का भंडारण न करें, वरना काला पड़कर खाने/बीज के लिए अनुपयुक्त हो जाती है।
- खरीफ मूंगफली:
- खरीफ मूंगफली की बुआई का उचित समय जून का दूसरा पखवाड़ा है। असिंचित क्षेत्रों में, जहां बुआई मानसून के बाद की जाती है, जुलाई के पहले पखवाड़े तक बुआई का काम पूरा कर लें।
- बुआई का तरीका:
- गुच्छेदार किस्मों के लिए: पंक्ति से पंक्ति 30 सें.मी. और पौधे से पौधे 10 सें.मी. की दूरी रखें। फैलने वाली प्रजातियों के लिए: पंक्ति से पंक्ति 45-60 सें.मी. और पौधे से पौधे 10-15 सें.मी. की दूरी रखें। खरीफ मौसम में, यदि संभव हो, तो मूंगफली की बुआई मेड़ों पर करें।
- मूंगफली की उन्नत प्रजातियाँ: ICGS-11, ICGS-44, ICCS-37, GG-3, GG-6, GG-12, VRI-2 आदि।
- बीज दर: मध्यम और अधिक फैलने वाली प्रजातियों के लिए: क्रमशः 80-100 किग्रा और 60-80 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर। गुच्छेदार किस्मों के लिए: 100-125 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है।
- बीज उपचार:
- बुआई से पहले बीज को 2 या 3 ग्राम थीरम या कार्बण्डाजिम प्रति किग्रा बीज की दर से शोधित करें।
- इस उपचार के 5-6 घंटे बाद, बीज को एक विशिष्ट प्रकार के उपयुक्त राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें।
- उपचार के बाद बीजों को छाया में सुखाएं और तुरंत बुआई के लिए उपयोग करें।
- पोषक तत्व:
- नाइट्रोजन यौगिकीकरण क्रिया के लिए : 20-30 किग्रा नाइट्रोजन, 40-60 किग्रा फॉस्फोरस, 30-40 किग्रा पोटाश/है.
- बारानी क्षेत्रों के लिए: 15-20 किग्रा नाइट्रोजन, 30-40 किग्रा फॉस्फोरस, 20-25 किग्रा पोटाश/है.
- गंधक व कैल्शियम हेतु: जिप्सम 200-400 किग्रा/है. (आधी बुआई और आधी फूल आने पर 5 सेमी गहराई में)।
- सूक्ष्म पोषक तत्व: 2 किग्रा बोरेक्स, 25 किग्रा जिंक सल्फेट/है.
गन्ना (Sugarcane)
- निराई-गुड़ाई, सिंचाई एवं पोषण:
- गन्ने की फसल में समय-समय पर निराई-गुड़ाई और सिंचाई करें।
- गन्ने की वृद्धि और उपज बढ़ाने के लिए यूरिया का छिड़काव 5% घोल के रूप में करें।
- नाइट्रोजन की शेष मात्रा (50 किग्रा/हेक्टेयर) टॉप ड्रेसिंग के रूप में डालकर मिट्टी चढ़ाएँ।
- यूरिया का प्रयोग बुआई के 45, 90, 120 और 150 दिन बाद करें।
- खरपतवार नियंत्रण: खरपतवार नियंत्रण हेतु हाथ से निराई करें। यदि मई में एट्राजिन का प्रयोग किया गया हो, तो इस माह 2,4-डी (1 किग्रा सक्रिय तत्व/हेक्टेयर) को 500–600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
सूरजमुखी (Sunflower)
- खरीफ सूरजमुखी:
- मृदा व तापमान:
- सूरजमुखी की खेती अच्छे जल निकास वाली दोमट व बलुई दोमट मृदा (pH 6.5–8.5) में बेहतर होती है। 26–30°C तापमान इसके लिए उपयुक्त है।
- बीज उपचार प्रक्रिया:
- बीजों को 1 लीटर पानी में 20 ग्राम ज़िंक सल्फेट घोल में 12 घंटे भिगोएँ।
- छाया में तब तक सुखाएँ जब तक बीजों में लगभग 8-9% नमी बच जाए।
- इसके बाद बाविस्टिन या थीरम से बीजों का उपचार करें।
- पुनः छाया में सुखाकर PSB (200 ग्राम/किग्रा बीज) से उपचारित करें।
- अंतिम बार बीजों को 24 घंटे छाया में सुखाएं।
- बुआई का समय:
- बीज उपचार के बाद 15 जून से बुआई करना उपयुक्त होता है।
- मृदा व तापमान:
- ग्रीष्मकालीन सूरजमुखी
- जब फूलों का पिछला भाग नींबू जैसा पीला हो और निचले पत्ते सूखने लगें, तब कटाई का सही समय होता है।
- सभी पत्तों के सूख जाने पर कटाई करें और फूलों को 2-3 दिन सुखाएं।
- बीज निकालने के लिए सूखे फूलों को लकड़ी या मशीन से पीटें।
- बीजों को भंडारण से पहले सुखाएं, ताकि नमी 10% से कम हो जाए।
- सूरजमुखी के डंठल दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी चारा होते हैं।
ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द(Summer Moong and Urad)
- फसल तब दैहिक रूप से परिपक्व मानी जाती है जब प्रकाश-संश्लेषित पदार्थों का आर्थिक भाग में स्थानांतरण रुक जाता है। जब 75-80% फलियाँ पक जाएं, तो उन्हें हंसिया से काट लेना चाहिए और एक-दो दिन के लिए खेत में ही सूखने देना चाहिए। कटाई में देरी करने पर फलियाँ चटक सकती हैं।
- कटाई के बाद मड़ाई करें और दानों को तब तक धूप में सुखाएं जब तक उनमें नमी 12% से कम न रह जाए। इसके बाद दानों को स्वच्छ और सूखे स्थान पर भंडारित करें।
- ग्रीष्मकालीन फसल की कटाई एक साथ की जाती है, लेकिन खरीफ फसल में कई बार बारिश के कारण एक साथ कटाई संभव नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में फलियों की तुड़ाई 2-3 बार की जा सकती है।
- इस विधि का उपयोग करके किसान मूंग और उड़द की अच्छी फसल उगा सकते हैं और प्रति हेक्टेयर 12-14 क्विंटल उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं।
अरहर (Pigeon Pea)
- अरहर की खेती के लिए मृदा:
- अरहर की अच्छी पैदावार के लिए ऐसी मृदा जरूरी है जिसमें जल निकास की व्यवस्था हो। खेत में पानी भरने से फसल को भारी नुकसान होता है। इसकी खेती के लिए मृदा का पीएच मान 5.5 से 8 के बीच होना चाहिए। लगातार एक ही खेत में अरहर नहीं उगानी चाहिए।
- बुआई का समय:
- बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई कर 2-3 बार हैरो चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। बुआई के समय खेत में नमी होना आवश्यक है। अरहर खरीफ की दलहनी फसल है, जिसे अगेती और पछेती रूप में उगाया जाता है। सिंचित क्षेत्रों में अगेती बुआई मध्य जून में करें और मेड़ों पर बोएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30-45 से.मी. और पौधे से पौधे की दूरी 5-10 से.मी. रखें। बुआई के लिए 15-18 कि.ग्रा./हेक्टेयर बीज पर्याप्त होता है। बीजों को 4-5 से.मी. गहराई में बोएं।
- बुआई की विधि एवं बीजोपचार
- मेडों पर बुआई करने से पैदावार बढ़ती है और जलभराव व रोगों से बचाव होता है। बीजों को बुआई से पहले 2-2.5 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बेण्डाजिम प्रति किलो बीज से उपचारित करें, फिर राइजोबियम कल्चर से बीजोपचार करें। पौधों की उचित संख्या होने से खरपतवारों की वृद्धि कम होती है और उत्पादन पर सकारात्मक असर पड़ता है।
- पोषक तत्व प्रबंधन:
- अच्छी उपज के लिए संतुलित उर्वरकों का प्रयोग आवश्यक है। प्रति हेक्टेयर 10-15 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 40-50 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 20 कि.ग्रा. सल्फर देना चाहिए। फॉस्फोरस हेतु 250 कि.ग्रा. सिंगल सुपर फॉस्फेट या 100 कि.ग्रा. डीएपी और 20 कि.ग्रा. सल्फर को पोरा या नाई की मदद से बीज के पास डालें, जिससे बीज को सीधे उर्वरक से संपर्क न हो। जहां जिंक की कमी हो, वहां 20 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर जिंक सल्फेट का प्रयोग करें।
कपास (Cotton)
- कपास की खेती एक लाभकारी फसल है, लेकिन इसे सफलतापूर्वक उगाने के लिए उपयुक्त समय, मृदा, बीजोपचार, पोषक तत्व प्रबंधन और रोग-कीट नियंत्रण की जानकारी होना जरूरी है।
- बुआई का समय एवं मृदा:
- अगर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो तो कपास की बुआई मई-जून में की जा सकती है। बुआई के लिए सीड-कम-फर्टी ड्रिल या प्लांटर का प्रयोग करना उपयुक्त होता है। कपास की खेती लगभग सभी प्रकार की मृदा में की जा सकती है, लेकिन रेतीली, लवणीय और सेम वाली मृदा उपयुक्त नहीं होती।
- फसल पद्धतिः फसल चक्र अपनाएं और प्रमाणित एवं रोग प्रतिरोधी बीजों का उपयोग करें। बीजोपचार अवश्य करें।
- बीजोपचार:
- बुआई से पहले बीजों को 2–5 ग्राम कार्बेन्डाजिम या कैप्टॉन प्रति किलोग्राम बीज से उपचारित करें। रस चूसक कीटों से बचाव के लिए प्रति किलोग्राम बीज पर 7 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड या 20 ग्राम कार्बोसल्फॉन का उपचार करें। दीमक से बचाव के लिए 10 लीटर पानी में 10 मिली क्लोरोपायरीफॉस मिलाकर बीज पर छिड़कें और छाया में सुखाकर बुआई करें।
- कपास की प्रमुख किस्में:
- संकर प्रजातियाँ — लक्ष्मी, एच.एस.45, एच.एस.6, एल.एच.144, एच.एल.1556, एफ.1861, एफ.1378, एफ.846।
- देसी प्रजातियाँ — एच.777, एच.डी.1, एच.974, एच.डी.107, एल.डी.327।
- बुआईः कपास की बुआई में पंक्तियों को अमेरिकी/देसी 60×30 सेमी, संकर 90×40 सेमी की दूरी में सीड ड्रिल या हल से करें, जिसमें अमेरिकन, संकर और देसी प्रजातियों के लिए क्रमशः 15-20, 4-5 और 10-12 कि.ग्रा./हैक्टर बीज की आवश्यकता होती है।
- पोषक तत्व प्रबंधन
- उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण की सिफारिशों के आधार पर करें।
- देसी किस्में: 50-70 किग्रा नाइट्रोजन, 20-30 किग्रा फॉस्फोरस प्रति हेक्टेयर।
- अमेरिकन एवं देसी किस्में: 60-80 किग्रा नाइट्रोजन, 30 किग्रा फॉस्फोरस, 20-30 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर।
- संकर किस्में: 150 किग्रा नाइट्रोजन, 60 किग्रा फॉस्फोरस और 60 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर।
- इसके अतिरिक्त, 25 किग्रा जिंक प्रति हेक्टेयर का प्रयोग लाभदायक है।
- उर्वरकों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण की सिफारिशों के आधार पर करें।
- रोग एवं कीट प्रबंधन:
- रोग नियंत्रण: कपास में बैक्टीरियल झुलसा रोग और फफूंदजनित रोग लगते हैं। इनके बचाव के लिए, वर्षा शुरू होने पर जून में 1.25 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% घुलनशील चूर्ण और 50 ग्राम एग्रीमाइसीन प्रति हेक्टेयर को 500-600 लीटर पानी में घोलकर 20-25 दिनों के अंतराल पर दो छिड़काव करें।
- कीट नियंत्रण: फुदका (जैसिड), सफेद मक्खी, माहू, तेला, थ्रिप्स और गूलरबेधक जैसे कीट कपास को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। इनके नियंत्रण के लिए:
- मोनोक्रोटोफॉस 25 ई.सी. 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर।
- सफेद मक्खी और गूलरबेधक कीट के लिए ट्राइकोफॉस 40 ई.सी. 1.50 लीटर प्रति हेक्टेयर। इन रसायनों को 250-300 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
चारा वाली फसलें (Fodder Crops)
- ज्वार: यदि आप ज्वार की बुवाई जून में करते हैं, खासकर जून के अंत में, तो इसके चारे में एच.सी.एन. (हाइड्रोसायनिक एसिड) का ज़हर कम बनता है। इससे पशुओं के बीमार होने का खतरा कम हो जाता है।
- मक्चरी: मक्चरी को भी 27 जून से 14 जुलाई तक बोया जा सकता है। इसे एक फुट की दूरी पर लाइनों में 16 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से बोएं।
- लोबिया और ग्वार: जून में आप लोबिया और ग्वार की बुवाई भी कर सकते हैं। ये दोनों भी पशुओं के लिए अच्छे चारे के विकल्प हैं।
- अप्रैल-मई में बोई गई फसलें: अप्रैल-मई में बोई गई चारा फसलों में पानी लगा दें। इससे फसल की कटाई जल्दी मिल सकेगी और पशुओं के लिए समय पर चारा उपलब्ध होगा।
हरी खाद वाली फसलें (Green Manure Crops)
- ढैंचा एक फलीदार फसल है जो हरी खाद बनाने के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है।
- हरी खाद के लिए: ढैंचा के 20 किलोग्राम बीज को 8 इंच की दूरी पर लाइनों में लगाएं।
- बीज उत्पादन के लिए: बीज की मात्रा आधी (10 किग्रा) कर दें और पौधों के बीच की दूरी दोगुनी (16 इंच) कर दें।
- बुवाई के समय 1.5 बोरे (लगभग 75 किग्रा) सिंगल सुपर फास्फेट डालें। यदि गेहूं में पहले ही फास्फोरस दिया गया है, तो इस खाद को दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है।
- हरी खाद वाली फसल को 3-4 बार सिंचाई दें। बुवाई के 55-60 दिन बाद, फसल को मिट्टी में अच्छी तरह मिला दें ताकि हरी खाद बन सके।
- हरी खाद बनाने के एक सप्ताह बाद, आप अपनी अगली फसल लगा सकते हैं।
सब्जियों की खेती (Vegetable Farming):
कद्दूवर्गीय फसलें (Cucurbitaceous Crops)
- कद्दूवर्गीय सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, करेला, टिंडा, कद्दू, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज और पेठा की बुवाई के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है।
- पोषक तत्व प्रबंधन: कद्दूवर्गीय सब्जियों में उर्वरकों का प्रयोग प्रजाति के अनुसार करें:
- उन्नत प्रजातियाँ: 50 किग्रा नाइट्रोजन, 25 किग्रा फॉस्फोरस और 25 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर।
- संकर प्रजातियाँ: 100 किग्रा नाइट्रोजन, 50 किग्रा फॉस्फोरस और 50 किग्रा पोटाश प्रति हेक्टेयर।
- बेल वाली फसलों में न्यूनतम नमी बनाए रखें, क्योंकि कम नमी पुष्पण (फूल आने) और परागण को प्रभावित कर सकती है, जिससे फसल उत्पादन में कमी आ सकती है।
- अधिक तापमान की आशंका को देखते हुए, तैयार सब्जियों की तुड़ाई सुबह या शाम को करें और उसके बाद उन्हें छायादार स्थान पर रखें।
भिंडी (Ladyfinger)
- भिंडी को लगभग सभी प्रकार की मृदा में उगाया जा सकता है, परंतु उच्च उत्पादन के लिए जल निकास की अच्छी व्यवस्था और जीवांशयुक्त 6.0 से 6.8 पीएच वाली दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। यदि इसकी बुआई अप्रैल-मई में की जाती है, तो तुड़ाई का समय जून में आता है। इस अवधि में तापमान अधिक होने के कारण सिंचाई प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। वर्तमान समय बरसाती भिंडी की बुआई के लिए उपयुक्त है।
- भिंडी की प्रमुख उन्नत प्रजातियों में पूसा ग्रीन भिंडी-5, पूसा ए-4, पूसा सावनी, पूसा मखमली, वर्षा उपहार, परभनी क्रांति, आजाद भिंडी, अर्का अनामिका, वीआरों-5 तथा वीआरों-6 शामिल हैं। एक हेक्टेयर खेत के लिए 8 से 10 किलोग्राम बीज पर्याप्त होते हैं, जिन्हें 45×30 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाता है।
- खेत की तैयारी करते समय 25 से 30 टन सड़ी गोबर की खाद या 10 टन नाडेप कम्पोस्ट प्रति हेक्टेयर मात्रा में खेत में मिलाना चाहिए। बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फॉस्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालना उचित रहता है। जब तुड़ाई शुरू हो जाए, तब 5 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया का प्रयोग करें और उसके तुरंत बाद सिंचाई करें।
- गर्मियों में तापमान अधिक होने के कारण हल्की और नियमित सिंचाई आवश्यक होती है। साथ ही, इस मौसम में माईट, जैसिड और हॉपर जैसे कीटों की निगरानी करते रहना चाहिए। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 30 से 60 दिनों के बीच 2 से 3 बार निराई-गुड़ाई करना पर्याप्त होता है। यदि खरपतवारों की समस्या अधिक हो, तो बुआई से पूर्व फ्लूक्लोरालिन 1.5 से 2.0 लीटर दवा को 500 से 600 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर छिड़काव करें।
टमाटर, बैंगन एवं मिर्च (Tomatoes, Brinjals and Chillies)
- बैंगन, टमाटर और मिर्च की पहले वाली फसलों में आवश्यकतानुसार सिंचाई और निराई-गुड़ाई करें।
- बैंगन:
- बैंगन की फसल को लंबे, गर्म और बरसाती मौसम की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकासी वाली सभी प्रकार की भूमि अच्छी पैदावार देती है। यदि मिट्टी दोमट और हल्की दोमट हो, तो यह इस फसल के लिए सबसे उपयुक्त होती है।
- पौधशाला में बीज बुवाई:
- बैंगन के लिए पौधशाला में 5-7 सें.मी. के फासलों से पंक्ति बनाकर बीज बोने चाहिए।
- सामान्य प्रजातियों के लिए एक हेक्टेयर हेतु 400-450 ग्राम बीज उपयुक्त होते हैं।
- संकर प्रजातियों के लिए 250-275 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त हैं।
- अगेती बैंगन की पौध तैयार करने के लिए पौधशाला की तैयारी कर बीज बोएं।
- बीज उपचार: बुवाई से पहले, प्रति किग्रा बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 ग्राम थीरम या कैप्टॉन से उपचारित करें।
- खरपतवार नियंत्रण: बैंगन की फसल में आवश्यकतानुसार 2-3 निराई-गुड़ाई करनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवारनाशी का भी उपयोग कर सकते हैं:
- इसके लिए एलाक्लोर 50 ईसी 3.5 लीटर या वासालिन 48 ईसी 2 लीटर प्रति हेक्टेयर को 800 से 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर रोपाई से पहले छिड़काव करना चाहिए।
- मिर्च:
- मिर्च की खेती मैदानी क्षेत्रों में वर्षा के मौसम में की जाती है। इसके लिए उपयुक्त तापमान इस प्रकार है: बीज अंकुरण के लिए 16−20°C, पौधे की बढ़वार के लिए 21−27°C, फल विकास एवं परिपक्वता के लिए 30°C है।
- खरीफ के मौसम में मिर्च की बुआई का समय जून-जुलाई तक होता है।
- बीज और पौध तैयारी:
- मिर्च के लिए 1000−1200 ग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर पर्याप्त है।
- अगेती मिर्च की पौध तैयार करने के लिए पौधशाला की तैयारी कर बीज बोएं।
- बुआई से पहले प्रति किलोग्राम बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 ग्राम थीरम या कैप्टॉन से उपचारित करें।
- हरी मिर्च की उपयुक्त प्रजातियाँ: पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार, एन.पी.-46 ए., पन्त सी-1 आदि।
- इस समय मिर्च की पौध भी तैयार होगी और जून के आखिरी समय तक 30−35 दिनों की पौध को खेत में रोपित कर देना चाहिए।
- रोपाई की दूरी: सामान्य प्रजातियाँ के लिए पंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी 45×45 सें.मी.। संकर प्रजातियाँ के लिएपंक्ति से पंक्ति एवं पौधे से पौधे की दूरी 60×45 सें.मी.।
- पोषक तत्व प्रबंधन: खेत की तैयारी करते समय 20−25 टन सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग करें। बुआई के समय 100−120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 60 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 40 कि.ग्रा. पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। रोपाई से पहले अंतिम जुताई के समय आधी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा मिट्टी में मिला दें। शेष नाइट्रोजन की मात्रा खड़ी फसल में दो बार में देनी चाहिए।
- रोग एवं सिंचाई प्रबंधन: मिर्च के खेत में विषाणु रोग से ग्रसित पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दें। इसके बाद इमिडाक्लोप्रिड 0.3 मिली/लीटर की दर से छिड़काव करें। आवश्यकतानुसार फसल में कम अंतराल पर सिंचाई करें।
फूलगोभी (Cauliflower)
- अगेती फूलगोभी की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। खेत को अच्छी तरह से जुताई करके और पाटा चलाकर तैयार करें।
- किस्मों का चयनः फूलगोभी की अगेती उन्नत किस्में: पूसा कार्तिक संकर, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिकी, पूसा अश्वनी, पूसा मेघना आदि प्रमुख हैं।
- बीज दर एवं बुआईः अच्छी जमाव क्षमता वाले बीज की दर 500-600 ग्राम/हेक्टेयर और संकर किस्मों के लिए 350-400 ग्राम/हेक्टेयर पर्याप्त है। फूलगोभी की अगेती बुआई के लिए मध्य मई से जून में बीज बोएं और 5-6 सप्ताह की पौध की रोपाई करें।
- पौधशाला तैयार करना और बीज बुवाई: लगभग 200 ग्राम बीज 2.5×1.0 मीटर आकार की सात क्यारियों में बोया जा सकता है।
- क्यारियों को 15 सें.मी. ऊंचा बनाएं। क्यारियों की लगभग 8 सें.मी. ऊपरी सतह पर सड़ी गोबर की खाद पर्याप्त मात्रा में मिलाएं और फिर क्यारी को समतल कर लें। बीज को 2.5−5.0 सें.मी. की पंक्तियों में बोना चाहिए। अगेती फूलगोभी की पौध तैयार करने के लिए सबसे पहले पौधशाला तैयार करें और फिर बीज बोएं।
- बीज उपचार के लिए 2 ग्राम बाविस्टीन/कैप्टॉन या 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किग्रा बीज करें।
- रोपाई की दूरी: अगेती फसल के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सें.मी. और पौधे से पौधे की दूरी 45 सें.मी. होनी चाहिए।
- पोषक तत्व प्रबंधनः खेत की तैयारी के समय 25-30 टन/हैक्टर गोबर की खाद मिलाएं। रोपाई से पहले 120 कि.ग्रा. नाइट्रोजन, 100 कि.ग्रा. फॉस्फोरस और 60 कि.ग्रा. पोटाश में से आधी नाइट्रोजन और पूरी फॉस्फोरस-पोटाश मिलाएं। शेष नाइट्रोजन को दो हिस्सों में बांटकर पहला हिस्सा रोपाई के एक महीने बाद और दूसरा हिस्सा फूल बनने के समय मिट्टी चढ़ाते समय डालें।
- खरपतवार नियंत्रण एवं जल प्रबंधनः खरपतवार नियंत्रण के लिए रोपाई से पहले 2.5 ली./है. बेसालीन या 3.3 ली./है. स्टॉम्प छिड़ककर हल्की सिंचाई करें; अगेती फसल में रोपाई के बाद साप्ताहिक, मध्यम/पछेती फसल में 10-15 दिन अंतराल पर सिंचाई करें।
- रोग प्रबंधनः फूलगोभी की नर्सरी में आर्द्रगलन रोग से बचाव के लिए बीज को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा या 2 ग्राम बाविस्टीन/कैप्टॉन प्रति किग्रा से उपचारित करें, या 25 ग्राम ट्राइकोडर्मा/10 किग्रा गोबर खाद 100 वर्ग मीटर नर्सरी में मिलाएं, या 2 ग्राम/लीटर बाविस्टीन/कैप्टॉन का छिड़काव करें।
अदरक और हल्दी
अदरक और हल्दी की फसल में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें और 50 किग्रा यूरिया प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें।
फलों की खेती (Fruit Farming):
- आम की बागवानी:
- आम के पौधों को सामान्यतः 10×10 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। हालांकि, सघन बागवानी के लिए इन्हें 2.5 से 4 मीटर की दूरी पर लगा सकते हैं। सघन बागवानी के लिए आम्रपाली और पूसा पीताम्बर जैसी किस्में सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं।
- गड्ढे की तैयारी और पौधा रोपण: पौधा लगाने से पहले खेत में रेखांकन कर पौधों का स्थान सुनिश्चित कर लें। पौधा लगाने के लिए 1×1×1 मीटर आकार का गड्ढा खोदें। वर्षा शुरू होने से पहले जून में, गड्ढों को 20-30 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, 2 किग्रा नीम की खली, 1 किग्रा हड्डी का चूरा या सिंगल सुपर फॉस्फेट और 100 ग्राम मिथाइल पैराथियॉन की डस्ट (10%) या 20 ग्राम थीमेट 10-जी के साथ खेत की ऊपरी सतह की मिट्टी मिलाकर अच्छी तरह भर दें। दो-तीन बार बारिश होने के बाद जब मिट्टी दब जाए, तब पूर्व चिन्हित स्थान पर खुरपी की सहायता से पौधे की पिंडी के आकार की जगह बनाकर पौधा लगाएं। पौधा लगाने के बाद आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर एक थाला बना दें और हल्की सिंचाई करें।
- पौधे की देखभाल: आम के पौधे की समुचित फलन और पूर्ण उत्पादन के लिए उसकी देखरेख आवश्यक है। पौधों को लगाने के बाद पूर्ण रूप से स्थापित होने तक सिंचाई करें। प्रारंभिक 2-3 वर्षों तक लू से बचाने के लिए सिंचाई करें। जमीन से 80 सें.मी. की ऊंचाई तक की शाखाओं को निकाल दें, जिससे मुख्य तने का समुचित विकास हो सके।
- ग्राफ्टिंग और कटाई-छंटाई: आम में ग्राफ्टिंग का कार्य इस माह शुरू करें। ग्राफ्टिंग के स्थान के नीचे से कोई शाखा नहीं निकलनी चाहिए। ऊपर की 3-4 शाखाओं को बढ़ने दें। बड़े और घने पेड़ों में, जो फल नहीं दे रहे हैं, उनकी बीच की शाखाओं को काट दें। फलों को तोड़ने के बाद, मंजर के साथ-साथ 2-3 सें.मी. टहनियों को काट दें ताकि स्वस्थ शाखाएं निकलें। ऐसा करने से अगले मौसम में अच्छा फलन प्राप्त होगा।
- कीट प्रबंधन: आम की डासी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल यूजीनॉल ट्रैप का प्रयोग करें। प्लाई/लकड़ी के टुकड़े को अल्कोहल, मिथाइल, मैलाथियान (6:4:1) के घोल में 48 घंटे डुबोने के बाद पेड़ पर लटका दें और ट्रैप को दो माह बाद बदल दें। मिलीबग की रोकथाम के लिए 2 प्रतिशत मिथाइल पैराथियॉन का उपयोग करना चाहिए।
- अमरूद:
- अमरूद के अच्छे उत्पादन के लिए उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इसके लिए मिट्टी का pH मान 6-7.5 उपयुक्त होता है, लेकिन pH मान 7.5 से ज़्यादा होने पर उकठा रोग का खतरा बढ़ जाता है। अमरूद को गर्म और उप-गर्म (उष्ण और उपोष्ण) जलवायु में सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। इसकी खेती के लिए 15-30 डिग्री सेल्सियस का तापमान अनुकूल है। यह सूखा भी अच्छी तरह सहन कर लेता है। ज़्यादा तापमान में उतार-चढ़ाव, गर्म हवा, कम बारिश, या जलभराव का फलों के उत्पादन पर ज़्यादा बुरा असर नहीं पड़ता है।
- अमरूद की उन्नत किस्में: सामान्य किस्में: इलाहाबाद सफेदा, हिसार सफेदा, लखनऊ-49, चित्तीदार, ग्वालियर-27, एपिल-गुवावा और धारीदार। व्यावसायिक उत्पादन के लिए: अर्का-मृदुला, श्वेता, ललित और पंत-प्रभात। संकर प्रजातियाँ: कोहीर, सफेदा और सफेद जाम।
- नए बागों का रोपण: नए बाग लगाने के लिए पहले निशान लगाएं और फिर गड्ढे खोदें। अमरूद के लिए 5×5 मीटर की दूरी पर 75 सेंटीमीटर लंबे, चौड़े और गहरे गड्ढे बनाएं। हर गड्ढे में 30-40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 1 किलोग्राम नीम की खली को ऊपर की मिट्टी में मिलाकर, गड्ढे को ज़मीन से 20 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक भर दें।
- शुरुआती 2-3 सालों में, बागों में खाली जगह पर खरीफ में लोबिया, ज्वार, उड़द, मूंग और सोयाबीन जैसी फसलें उगा सकते हैं।
- आंवला:
- आंवला एक बहुत ही उत्पादनशील पौधा है जिसमें ढेर सारे पोषक तत्व और औषधीय गुण होते हैं। यह विटामिन ‘सी’ का एक मुख्य स्रोत है और इसमें शर्करा व अन्य पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आंवला उष्ण जलवायु का पौधा है, लेकिन इसकी खासियत यह है कि इसे शुष्क प्रदेशों में भी आसानी से उगाया जा सकता है।
- मिट्टी और pH मान: बलुई मिट्टी को छोड़कर आंवले की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यह पौधा काफी कठोर होता है, इसलिए इसे 9 तक के pH मान वाली सामान्य मिट्टी में भी उगाया जा सकता है।
- ऊसर (क्षारीय) मिट्टी में गड्ढा तैयार करना (जून में): अगर आप ऊसर मिट्टी में खेती कर रहे हैं, तो जून में 8-10 मीटर की दूरी पर 1.0-1.25 मीटर के गड्ढे खोद लें। बरसात के मौसम में इन गड्ढों में पानी भर दें। इकट्ठा हुए पानी को निकालकर फेंक दें। प्रत्येक गड्ढे में 50-60 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, 15-20 किग्रा बालू, 8-10 किग्रा जिप्सम और लगभग 5 किग्रा ऑर्गेनिक खाद का मिश्रण भर दें। भराई के 15-25 दिनों बाद, जब अभिक्रिया समाप्त हो जाए, तभी पौधे का रोपण करें।
- सामान्य मिट्टी में गड्ढा तैयार करना: सामान्य मिट्टी में प्रत्येक गड्ढे में 40-50 किग्रा सड़ी गोबर की खाद और 2 किग्रा नीम की सड़ी खाद का मिश्रण, ऊपर वाली मिट्टी के साथ मिलाकर भर दें। गड्ढों को जमीन की सतह से 15-20 सें.मी. ऊंचाई तक भरें।
- पपीता:
- पपीते की अच्छी खेती के लिए गर्म और नमीयुक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। इसे अधिकतम 38-44 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान पर उगाया जा सकता है। उपजाऊ जमीन, जिसमें जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो, पपीते की खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। पपीते के नए बाग लगाने के लिए, पहले निशान लगाएं और फिर गड्ढे खोदें।
- गड्ढे की तैयारी और रोपण: पपीते के लिए 2.1-5 मीटर की दूरी पर 75 सें.मी. लंबे, चौड़े और गहरे गड्ढे बनाएं। प्रत्येक गड्ढे में 30-40 किग्रा सड़ी गोबर की खाद और 1 किग्रा नीम की खली को गड्ढे से निकाली गई ऊपरी मिट्टी में मिलाकर, गड्ढे को जमीन से 20 सें.मी. की ऊंचाई तक भर दें।
- बीज और पौध तैयार करना: एक हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम से 1 किग्रा बीज की आवश्यकता होती है। पपीते के पौधे बीज द्वारा तैयार किए जाते हैं। एक हेक्टेयर खेती में प्रति गड्ढे 2 पौधे लगाने पर लगभग 5000 पौधों की आवश्यकता होती है।
- पपीते की उन्नत किस्में: पूसा मेजस्टी, पूसा जॉयंट, पूसा डिलीशियस, वाशिंगटन, सोलो, हनीड्यू, कुर्ग हनीड्यू, कोयम्बटूर, पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्हा, सिलोन।
- पौध तैयार करना: 20 सें.मी. चौड़े मुंह वाली, 25 सें.मी. लंबी और 150 सें.मी. छेद वाले पॉलीथीन थैले लें। इन थैलों में गोबर की खाद, मिट्टी और रेत का मिश्रण भरें। थैली का ऊपरी 1 सें.मी. भाग खाली छोड़ दें। प्रति थैली 2 से 3 बीज होने चाहिए। मिट्टी में हमेशा पर्याप्त नमी बनाए रखें।
- रोपण: जब पौधे 15−20 सें.मी. ऊंचे हो जाएं, तब थैलियों को नीचे से धारदार ब्लेड द्वारा सावधानीपूर्वक काटकर, पहले से तैयार किए गए गड्ढों में लगाएं।
- नींबू के पौधों में उर्वरक प्रबंधन के लिए, पहले साल से ही 25 ग्राम नाइट्रोजन और 25 ग्राम पोटाश देना शुरू करें। इस मात्रा को हर साल बढ़ाते रहें, जब तक कि यह 10 साल या उससे अधिक उम्र के पौधों के लिए 250 ग्राम नाइट्रोजन और पोटाश न हो जाए। यह उर्वरक आप जून माह में या फल लगने के दो महीने बाद डाल सकते हैं।
- लीची एक स्वादिष्ट और महत्वपूर्ण फल है, और इसका प्रवर्धन मुख्य रूप से गूटी (लेयरिंग) द्वारा किया जाता है। जून का दूसरा पखवाड़ा गूटी द्वारा प्रवर्धन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। इस महीने में बांधी गई गूटी से सर्वाधिक सफलता मिलती है।
- अंगूर को जल्दी तैयार करने और उसकी मिठास बढ़ाने के लिए, पकने से 15 दिन पहले 50 मिलीलीटर इथिफॉन और 100 ग्राम बोरेक्स को 100 लीटर पानी में घोलकर पौधों पर छिड़काव करें। इस छिड़काव के बाद सिंचाई न करें।
- बेर: बेर के पौधों को अच्छी तरह विकसित करने और बेहतर उत्पादन के लिए सही मात्रा में उर्वरक देना और समय पर कटाई-छंटाई करना ज़रूरी है।
- उर्वरक प्रबंधन:
- एक वर्ष के पौधे: हर पौधे को 5.0 किग्रा सड़ी गोबर की खाद, 50 ग्राम नाइट्रोजन, 50 ग्राम फॉस्फोरस और 25 ग्राम पोटाश दें।
- आठ वर्ष तक वृद्धि: इस मात्रा को हर साल इसी अनुपात में बढ़ाते रहें।
- आठ वर्ष या उससे अधिक आयु के पौधे: प्रति पौधे 40 किग्रा गोबर की सड़ी खाद, 400 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फॉस्फोरस और 250 ग्राम पोटाश का प्रयोग करें।
- कटाई एवं छंटाई: बेर में कटाई और छंटाई का काम समय से पूरा करें। यह पौधों की वृद्धि, फलने और समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है।
- उर्वरक प्रबंधन:
- केला: केले की रोपाई के लिए यह उपयुक्त समय है।
- मृदा और जलवायु: केले उगाने के लिए, अच्छे निकास वाली, पर्याप्त उपजाऊ और नमी धारण करने की क्षमता वाली मृदा का चयन करें। उच्च नाइट्रोजन, पर्याप्त फॉस्फोरस और उच्च पोटाश स्तर वाली मृदा में केले की खेती अच्छी होती है। जल जमाव, कम हवादार, कम पौष्टिक तत्वों वाली, रेतीली, नमक वाली, कैल्शियम युक्त और अत्यधिक चिकनी मृदा में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए।
- खेत की तैयारी: गर्मियों में, कम से कम 3 से 4 बार जुताई करें। आखिरी जुताई के समय, 10 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद या गाय का सड़ा हुआ गोबर मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। जमीन को समतल करने के लिए ब्लेड हैरो या लेजर लेवलर का प्रयोग करें। वे क्षेत्र जहाँ निमाटोड की समस्या होती है, वहाँ पर रोपाई से पहले निमाटीसाइड और धूम्रक (fumigant) गड्ढों में डालें।
- बुवाई का समय और रोपण: बिजाई के लिए मध्य फरवरी से मार्च का पहला सप्ताह उपयुक्त होता है। उत्तरी भारत में तटीय क्षेत्रों में, जहाँ उच्च नमी और तापमान 5-7 डिग्री सेल्सियस से कम न हो, वहाँ पर रोपाई के लिए 1.8 मीटर × 1.8 मीटर से कम फासला नहीं होना चाहिए। केले की जड़ों को 45×45×45 सें.मी. या 60×60×60 सें.मी. आकार के गड्ढों में रोपित करें। गड्ढों को धूप में खुला छोड़ें ताकि हानिकारक कीट नष्ट हो जाएं।गड्ढों को 10 किग्रा गोबर की खाद या सड़ा हुआ गोबर, 250 ग्राम नीम खली और 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन से भरें। जड़ों को गड्ढे के मध्य में रोपित करें और मिट्टी को आसपास अच्छी तरह से दबाएं। गहरी रोपाई न करें।
- पौधों की संख्या: यदि 1.8 मीटर × 1.8 मीटर का फासला लिया जाए, तो प्रति एकड़ 1452 पौधे लगाएं। यदि 2 मीटर × 2.5 मीटर का फासला लिया जाए, तो एक एकड़ में 800 पौधे लगाने की सिफारिश की जाती है।
- बीजोपचार / राइजोम उपचार: रोपाई के लिए, सेहतमंद और संक्रमण रहित जड़ों या राइजोम का प्रयोग करें। रोपाई से पहले, जड़ों को धोएं और क्लोरोपाइरीफॉस 20 ईसी 2.5 मि.ली. प्रति लीटर पानी में डुबोएं। फसल को राइजोम की सूंडी से बचाने के लिए रोपाई से पहले कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी 33 ग्राम में जड़ों को डुबोएं और उसके बाद 72 घंटों के लिए छांव में सुखाएं। गांठों को निमाटोड के प्रकोप से बचाने के लिए कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी 50 ग्राम प्रति जड़ का उपचार करें। फ्यूजेरियम की रोकथाम के लिए, जड़ों को कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में 15-20 मिनट के लिए डुबोएं।
- सिंचाई: केले की फसल को अच्छी उपज के लिए 70-75 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। सर्दियों में 7-8 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। गर्मियों में 4-5 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। बारिश के मौसम में आवश्यकतानुसार सिंचाई करें। अतिरिक्त पानी को खेत में से निकाल दें क्योंकि यह पौधों की नींव और वृद्धि को प्रभावित करेगा। टपक सिंचाई (ड्रिप इरिगेशन) का प्रयोग करें; यह 58% पानी बचाता है और 23-32% उपज बढ़ाता है।
- कीटों की रोकथाम:
- फल की सूंडी: यदि प्रकोप दिखे, तो तने के चारों तरफ मिट्टी में कार्बरिल 10-20 ग्राम प्रति पौधे में डालें।
- राइजोम की सूंडी: रोकथाम के लिए सूखे हुए पत्तों को निकाल दें और बाग को साफ रखें। रोपाई से पहले राइजोम को मिथाइल ऑक्सीडेमेटन 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में डुबो दें। रोपाई से पहले अरंडी की खली 250 ग्राम या कार्बरिल 50 ग्राम या फोरेट 10 ग्राम प्रति गड्ढे में डालें।
- चंपा: यदि प्रकोप दिखे तो मिथाइल डेमेटन 2 मि.ली. या डाइमेथोएट 30 ईसी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- थ्रिप्स: रोकथाम के लिए मिथाइल डेमेटन 20 ईसी 2 मि.ली. या मोनोक्रोटोफॉस 36 डब्ल्यूएससी 2 मि.ली. प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें।
- निमाटोड: जड़ों को निमाटोड के प्रकोप से बचाने के लिए, कार्बोफ्यूरॉन 3% सीजी, 504 ग्राम प्रति जड़ का उपचार करें। यदि जड़ का उपचार न किया गया हो, तो रोपाई के एक महीने बाद कार्बोफ्यूरॉन पौधे के चारों तरफ डालें।
औषधीय फसलें (Medicinal Crops)
- मेंथा: महीने के अंत में मेंथा की दूसरी कटाई कर लें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें।
फूल और सुगंधित पौधे (Flowers and Fragrant Plants):
- गुलदाउदी की कटिंग तैयार करें।
- गेंदा, देसी गुलाब, ग्लैडियोलस और रजनीगंधा में नियमित रूप से निराई-गुड़ाई करें और आवश्यकतानुसार सिंचाई का ध्यान रखें।
- बेहतर फूलों के लिए: फूलों की संख्या और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड (जी. ए.3) 50 मि.ग्रा. प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
- लिली और बेला में भी आवश्यकतानुसार सिंचाई और निराई-गुड़ाई करते रहें।
पशुपालन/दुग्ध विकास (Animal Husbandry/Dairy Development):
- टीकाकरण: अपने सभी पशुओं को गलघोटू (Haemorrhagic Septicaemia) और लंगड़िया बुखार (Black Quarter) का टीका ज़रूर लगवाएं। यह इन गंभीर बीमारियों से बचाव के लिए अत्यंत आवश्यक है।
- लू से बचाव: पशुओं को तेज गर्मी और लू से बचाएं। उन्हें छायादार स्थान पर रखें और पर्याप्त हवादार जगह उपलब्ध कराएं।
- हरे चारे की व्यवस्था: पशुओं को पर्याप्त मात्रा में हरा चारा दें। यह उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उन्हें स्वस्थ रखता है। परजीवी नियंत्रण: पशुओं को परजीवी की दवा पिलाएं। यह आंतरिक परजीवियों से मुक्ति दिलाएगा और उनके स्वास्थ्य को सुधारेगा।
- चारागाह की तैयारी:खरीफ के चारे जैसे मक्का और लोबिया के लिए खेत की तैयारी शुरू कर दें।
- बांझपन का उपचार: यदि कोई पशु बांझ (अनुत्पादक) है, तो उसका तुरंत उपचार कराएं।
- सूखे चारे से बचें: सूखे खेत से चरी (ज्वार या बाजरे का सूखा चारा) न खिलाएं, क्योंकि इसमें जहर (हाइड्रोसायनिक एसिड) फैलने का डर रहता है, जो पशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है।
मुर्गी पालन (Poultry Farming):
- मुर्गियों को गर्मी से बचाने के लिए पर्दों पर पानी के छींटे मारें और उन्हें लगातार स्वच्छ पानी उपलब्ध कराएं।